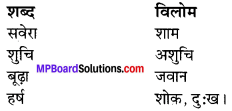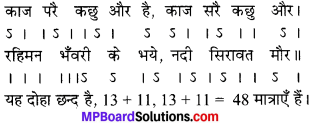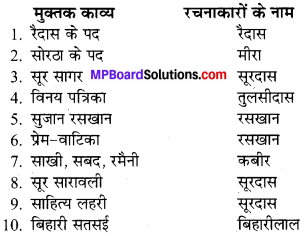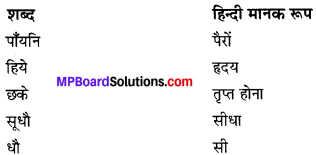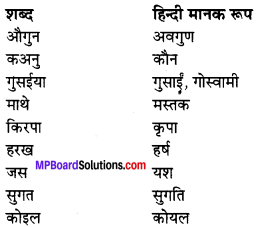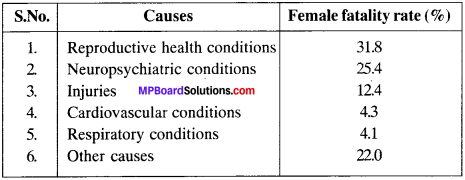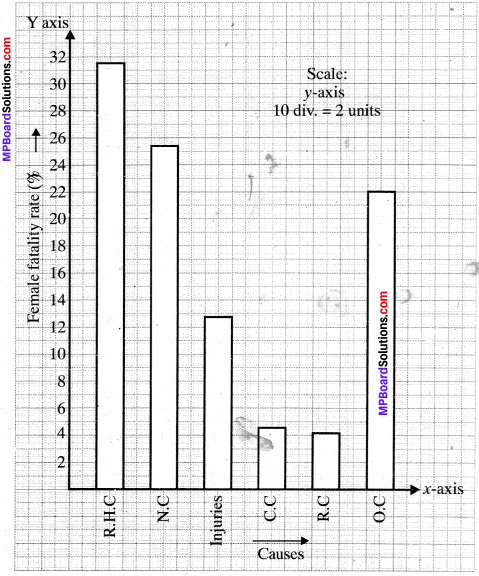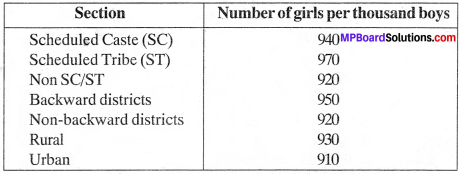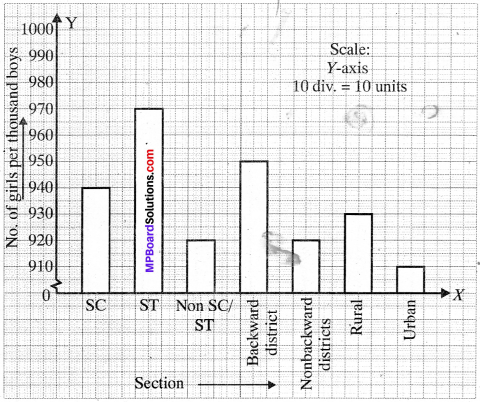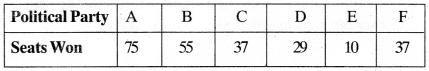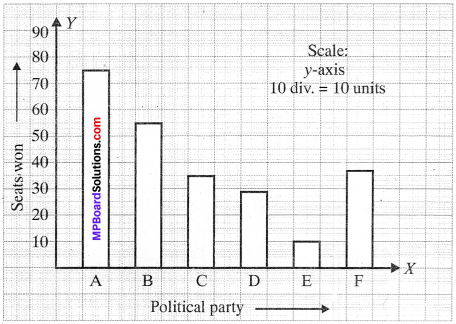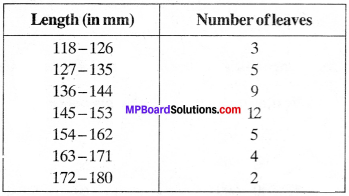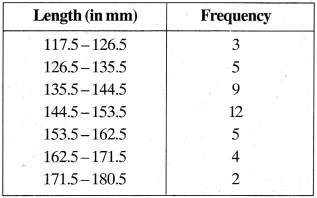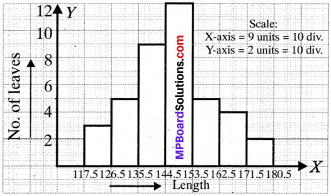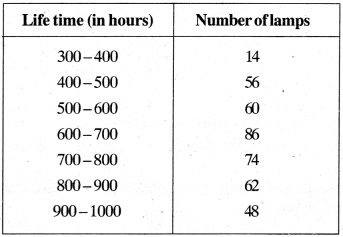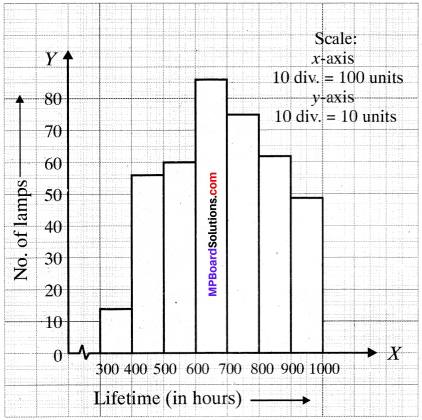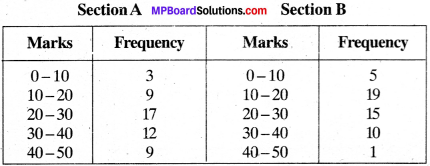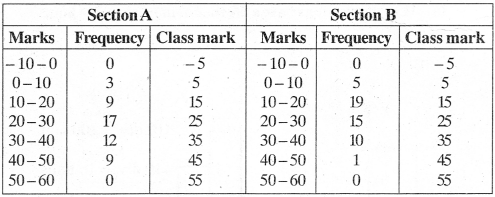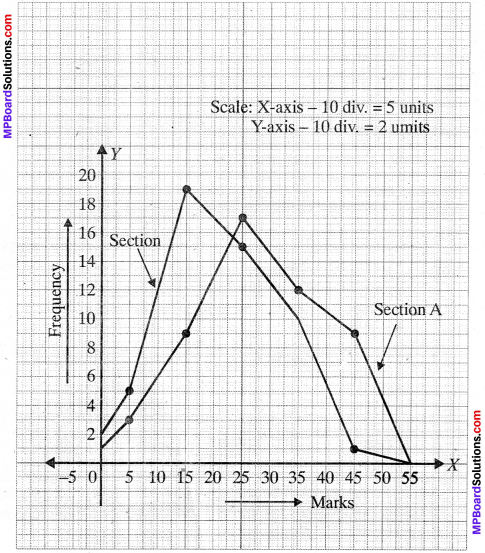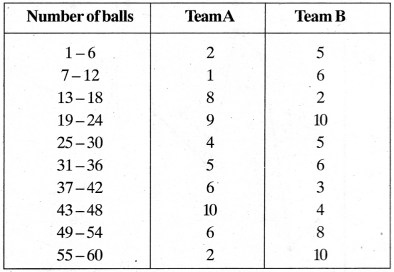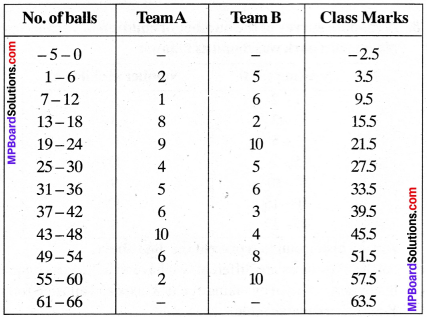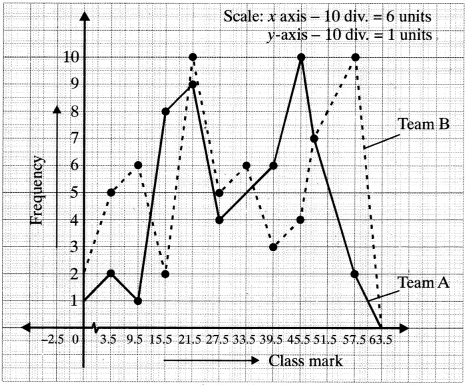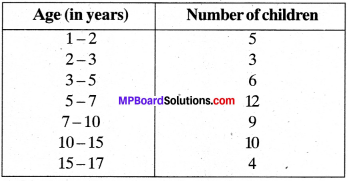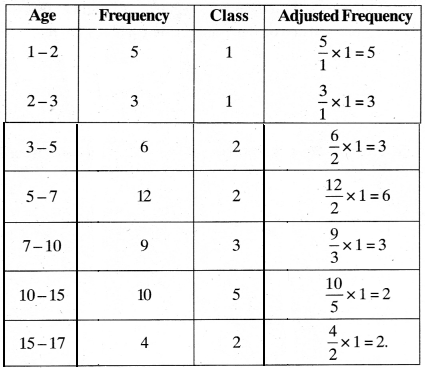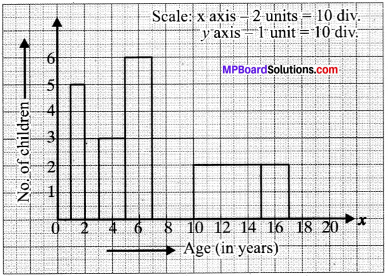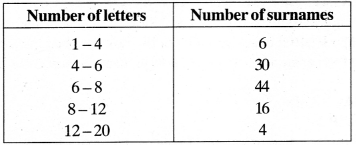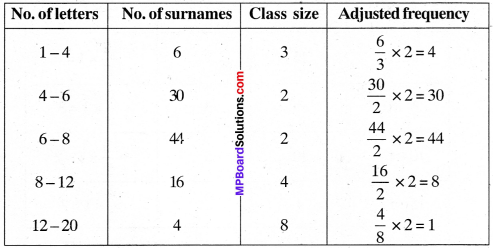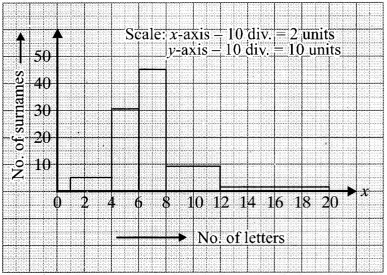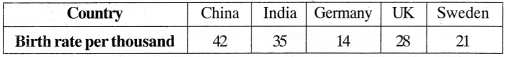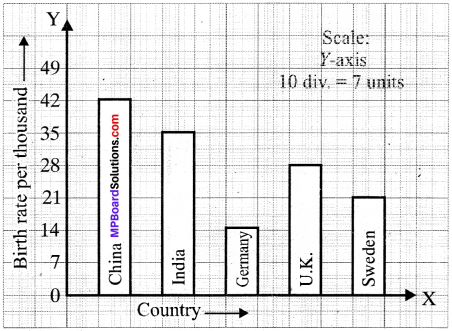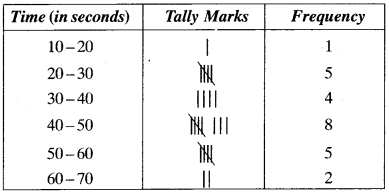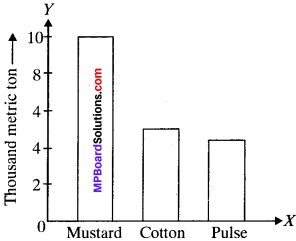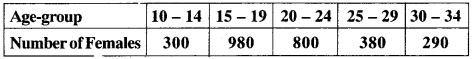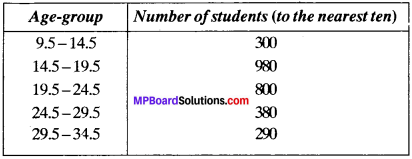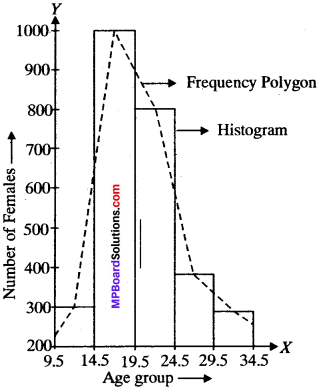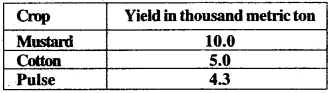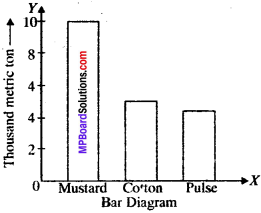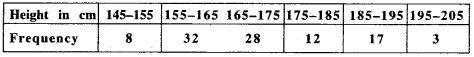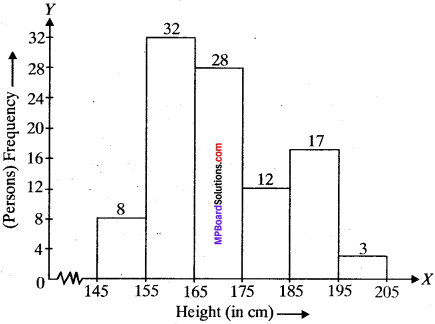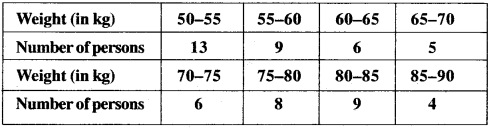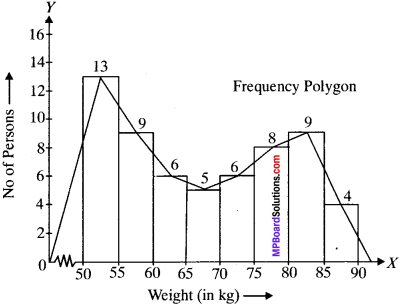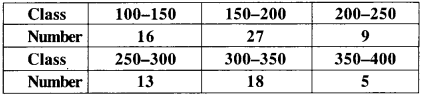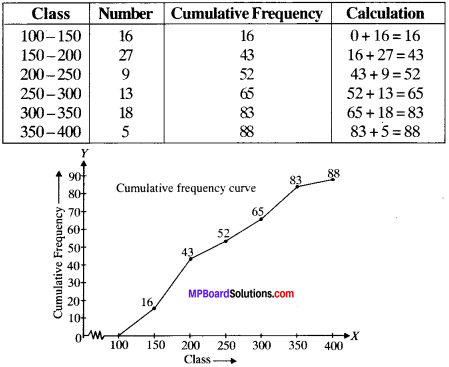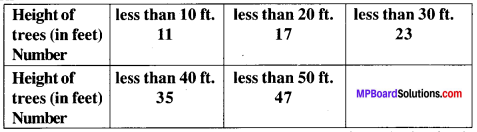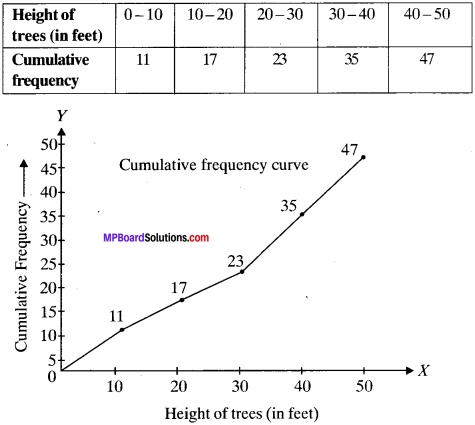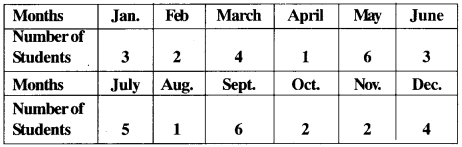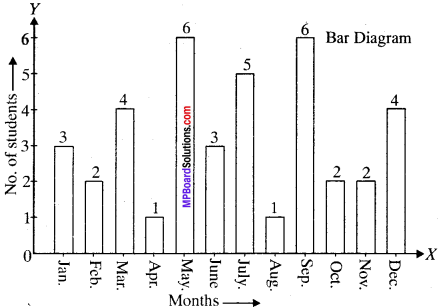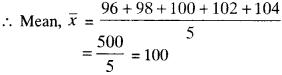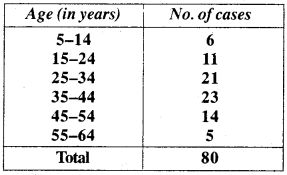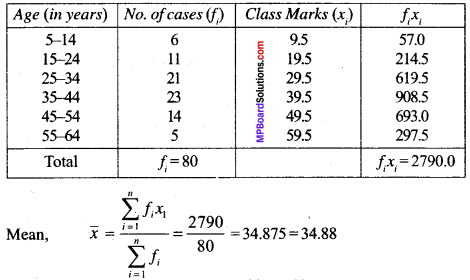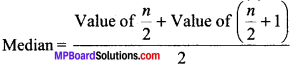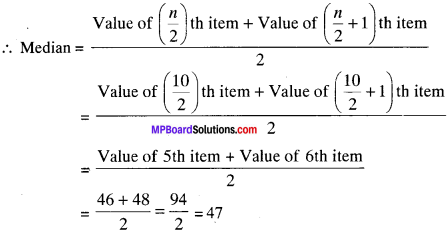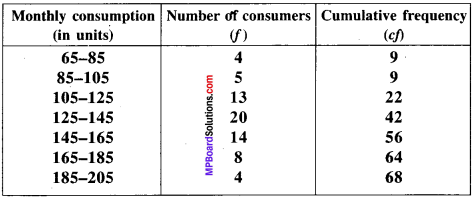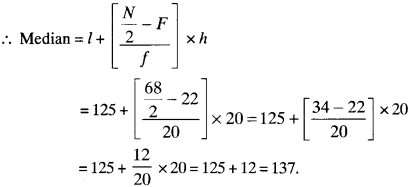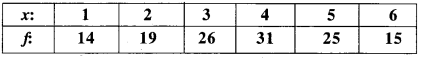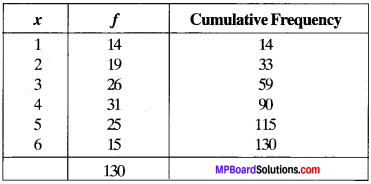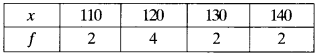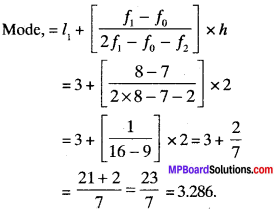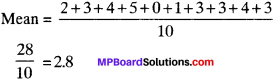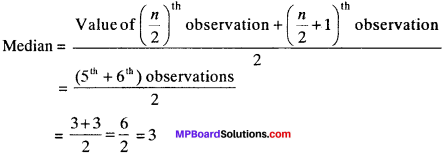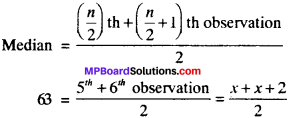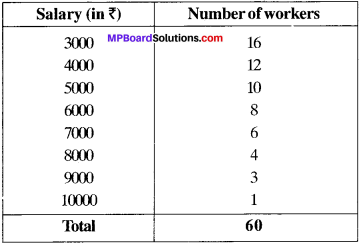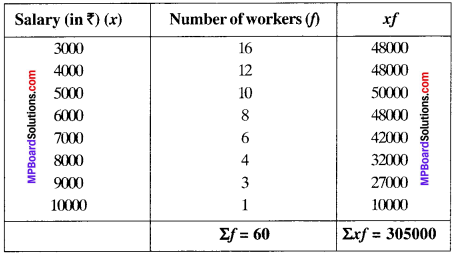MP Board Class 9th Hindi Navneet Solutions पद्य Chapter 8 कल्याण की राह
कल्याण की राह अभ्यास
बोध प्रश्न
कल्याण की राह अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
कवि ‘मन’ में किस बात के लिए इंगित करते
उत्तर:
कवि ‘मन’ में इस बात के लिए इंगित करते हैं कि हमारा विश्वास सूरज के चक्र के समान सदैव गतिशील बना रहे।
प्रश्न 2.
कवि किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात करता है?
उत्तर:
कवि विश्वास एवं प्रगति चक्र को नहीं रुकने देने की बात करता है।
प्रश्न 3.
तुलसीदास एवं गिरिजाकुमार माथुर की दो अन्य कविताओं के नाम लिखिए।
उत्तर:
तुलसीदास जी ने ‘विनय-पत्रिका’ एवं ‘दोहावली’ नामक रचनाएँ लिखी हैं। गिरिजाकुमार माथुर ने ‘धूप के धान’ तथा ‘नाश और निर्माण’ नामक कृतियाँ रची हैं।
प्रश्न 4.
‘तात राम नर नहीं भूपाला’ कथन किसने किससे कहा?
उत्तर:
यह कथन विभीषण ने रावण से कहा है।
प्रश्न 5.
माल्यवन्त कौन था?
उत्तर:
माल्यवन्त रावण का सचिव (मंत्री) था।
![]()
कल्याण की राह लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
विभीषण रावण से बार-बार क्या विनती करता है?
उत्तर:
विभीषण रावण से बार-बार विनती करता है कि हे तात! यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सीताजी को राम को वापस दे दीजिए, राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। वे तो काल के भी काल हैं, दीनबन्धु हैं और शरणागत शत्रु की रक्षा करने वाले हैं अतः आप मेरी बात मान जाइए और सीताजी को उन्हें वापस लौटा दीजिए।
प्रश्न 2.
“सीता देहु राम कहुँ अहित न होय तुम्हार” से क्या आशय है?
उत्तर:
विभीषण रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे तात! मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर विनती करता हूँ कि तुम्हें मेरे दुलार की (छोटे भाई-बहन के प्रति बड़ों का स्नेह अथवा कल्याण की भावना) रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें श्रीराम को उनकी सीता को लौटा देना चाहिए इससे तुम्हारा किसी भी दशा में अहित नहीं होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि सीता राक्षसों के कुल के लिए काल सिद्ध होगी।
प्रश्न 3.
“पाँव में अनीति के मनुष्य कभी झुके नहीं” का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
गिरिजाकुमार माथुर का इस पंक्ति से आशय यही है कि मनुष्य को कभी अनीति और अन्याय के मार्ग पर अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। अनीति और अन्याय करने से मनुष्य की अच्छी वृत्तियों के विकास में बाधा पड़ती है। अपने जीवन के लक्ष्य को नीति का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है।
कल्याण की राह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
विभीषण के समझाने पर रावण ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की?
उत्तर:
विभीषण ने जब रावण से कहा कि उसे राम से बैर मोल नहीं लेना चाहिए। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। उनसे शत्रुता करके कोई बच नहीं सकता। अत: बैर भाव छोड़कर उन्हें सीता सौंपकर उनकी शरण में चले जाओ। वे शरणागत वत्सल हैं। वे तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार जब विभीषण ने रावण को समझाया तो रावण पर इसकी विपरीत ही प्रतिक्रिया हुई। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला कि तुम शत्रु के उत्कर्ष की बात करते हो, शत्रु का गुणगान करते हो। अरे कोई है जो इन दोनों को (विभीषण और माल्यवन्त को) राजसभा से दूर कर दे। इतना सुनकर माल्यवन्त तो उठकर अपने घर चला गया। किन्तु विभीषण ने फिर भी हार नहीं मानी। वह उसे पुनः समझाने का प्रयास करने लगा। इस पर रावण ने उस पर अपने पाँव से आघात किया। तब दु:खी होकर और मन में रावण का सर्वनाश विचार कर विभीषण राम की शरण में आ गया।
प्रश्न 2.
‘सूरज का पहिया’ से कवि का क्या आशय है?
उत्तर:
‘सूरज का पहिया’ से कवि का यह आशय है कि जिस प्रकार सूरज का पहिया बिना थके, बिना रुके रात-दिन चलता रहता है उसी तरह मनुष्य को भी मन के विश्वास के स्वर्णिम चक्र को चलाए रखना चाहिए। उसे अपने विश्वास को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। सूर्य की भाँति न तो उसकी आभा मन्द होनी चाहिए और न गति रुकनी चाहिए।
प्रश्न 3.
‘विभीषण-रावण संवाद’ एवं ‘सूरज का पहिया’ कविताएँ कल्याण की राह बताती हैं। स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
‘विभीषण-रावण संवाद’ कविता में विभीषण ने रावण को बार-बार समझाया है कि हे तात! तुम कुबुद्धि को त्याग दो क्योंकि कुबुद्धि विपत्तियों का घर होती है और उससे मानव का कुछ भला नहीं होता है। अत: सुमति को अपनाओ और पर स्त्री को श्रीराम को सौंपकर उनकी शरण ले लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
‘सूरज का पहिया’ कविता भी मानव के कल्याण की बात करती है। मानव को सूर्य के समान सदैव आभा युक्त होकर बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर आगे बढ़ता रहना चाहिए।
प्रश्न 4.
सूरज की तश्तरी’ से कवि का क्या आशय है?
उत्तर:
‘सूरज की तश्तरी’ से कवि का आशय है कि मानव जीवन भर सूर्य के समानं संसार को ज्ञान (प्रकाश) बाँटता रहे। वह कभी थके नहीं, रुके नहीं। उसके होठों पर अपने विश्वास के गीत हों और भविष्य निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाए। सूरज की तश्तरी के समान ही उसकी चमक कभी कम न होने पाए।
![]()
कल्याण की राह काव्य-सौन्दर्य
प्रश्न 1.
सन्दर्भ सहित व्याख्या कीजिए
(1) सचिव वैद गुरु………….बेगिही नास।
उत्तर:
कविवर तुलसीदास का कथन है कि मंत्री, वैद्य और गुरु यदि भय के कारण प्रिय लगने वाला झूठ बोलते हैं अर्थात् चापलूसीवश सत्य बात न बोलकर मीठी बातें बोलते हैं तो इनसे क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहने का भाव यह है कि यदि मंत्री राज्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन न करके राजा को झूठी खबर या सूचना देता है, यदि वैद्य रोगी की वास्तविक दशा को न बताकर झूठ बोलता है और यदि गुरु भयवश (या स्वार्थवश) धर्म की बात नहीं बोलता है तो इन स्थितियों में क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए।
किन्तु रावण की राजसभा में तो यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय उपयुक्त अवसर समझकर विभीषण वहाँ आ गया। उसने भाई के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरान्त सिर को झुकाकर पुनः प्रणाम करके अपने आसन पर बैठकर और रावण से आज्ञा पाकर इस प्रकार वचन बोला-हे दयामय! आप यदि मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हितकारी बात को कहना चाहता हूँ। हे तात! यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप सुन्दर कीर्ति, सुन्दर बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं तो आप पराई स्त्री के मस्तक को चौथ के चन्द्रमा की भाँति कलंक युक्त मानते हुए उसका परित्याग कर दें।
अर्थात् जिस प्रकार भाद्रपद मास में कृष्णपक्ष की चतुर्थी का चन्द्र दर्शन कलंक का कारण बनता है, उसी भाँति पराई स्त्री को घर में रखना कलंक का कारण है। अतः पराई स्त्री का त्याग करना ही उचित है। अत: तुम श्रीराम की पत्नी सीता को उन्हें वापस लौटा दो। वे चौदह लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके कोई बच नहीं सकता। हे स्वामी! मनुष्य के लिए काम वासना, क्रोध, अहंकार, लिप्सा ये सब नरक के मार्ग हैं अर्थात् इनसे व्यक्ति को नरक का मुँह देखना पड़ता है। अतः इन सबका त्याग करके सीता को राम को सौंपकर उनका भजन करो, जिनका भजन साधु सन्त करते रहते हैं अर्थात् उन श्रीराम की भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है।
(2) मन में विश्वास …………. चुके नहीं।
उत्तर:
कविवर श्री गिरिजाकुमार माथुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के विश्वास को सदैव मजबूत बनाये रखना चाहिए। वह निरन्तर स्वर्णिम चक्र की भाँति (सूर्य के गोले के समान) निरन्तर गतिशील बना रहना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारे मन में पीली केसर की भाँति जो स्वप्न जन्म ले रहे हैं, वे कभी चुक न जाएँ अर्थात् समाप्त न हो जाएँ। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे मन में जो स्वप्न जन्मे हैं वे सदैव पल्लवित और पुष्पित होते रहें, वे कभी मुरझाएँ नहीं। तुम अपने जीवन में सदैव उसी तरह प्रकाशित होते रहो जिस तरह सूर्य का गोला प्रकाशित होता रहता है।
अतीत के डंठलों पर भविष्य के चन्दनों को उगाओ। कहने का भाव यह है कि अतीत में तुमने अनेकानेक संकट एवं विपत्तियाँ झेली हैं पर अपने भविष्य को तुम चन्दन के समान महकाओ। तुम्हारी आँखों में तुम्हारे विश्वास की रंग-बिरंगी तस्वीर हो। तुम्हारे ओठों पर तुम्हारे स्वप्नों के गीत हों। यदि कभी तुम्हारे जीवन में शाम भी आ जाए अर्थात् निराशा आ जाए तब भी तुम चन्द्रमा के समान अपनी शीतलता बिखेरते रहना। कहने का भाव यह है कि निराशा में भी अपनी आशा का संबल मत छोड़ना। तुम्हारी आँखों की बरौनियों में चन्द्रमा कभी भी थके नहीं अपितु वह निरन्तर गतिशील बना रहे। तुम्हारे जीवन के स्वप्नों की पीली केसर कभी भी मुरझाए नहीं, ऐसा तुम्हें सदैव प्रयत्न करना चाहिए।
(3) काम क्रोध………………जेहि संत।
उत्तर :
किन्तु रावण की राजसभा में तो यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय उपयुक्त अवसर समझकर विभीषण वहाँ आ गया। उसने भाई के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरान्त सिर को झुकाकर पुनः प्रणाम करके अपने आसन पर बैठकर और रावण से आज्ञा पाकर इस प्रकार वचन बोला-हे दयामय! आप यदि मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हितकारी बात को कहना चाहता हूँ। हे तात! यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप सुन्दर कीर्ति, सुन्दर बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं तो आप पराई स्त्री के मस्तक को चौथ के चन्द्रमा की भाँति कलंक युक्त मानते हुए उसका परित्याग कर दें।
अर्थात् जिस प्रकार भाद्रपद मास में कृष्णपक्ष की चतुर्थी का चन्द्र दर्शन कलंक का कारण बनता है, उसी भाँति पराई स्त्री को घर में रखना कलंक का कारण है। अतः पराई स्त्री का त्याग करना ही उचित है। अत: तुम श्रीराम की पत्नी सीता को उन्हें वापस लौटा दो। वे चौदह लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके कोई बच नहीं सकता। हे स्वामी! मनुष्य के लिए काम वासना, क्रोध, अहंकार, लिप्सा ये सब नरक के मार्ग हैं अर्थात् इनसे व्यक्ति को नरक का मुँह देखना पड़ता है। अतः इन सबका त्याग करके सीता को राम को सौंपकर उनका भजन करो, जिनका भजन साधु सन्त करते रहते हैं अर्थात् उन श्रीराम की भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है।
प्रश्न 2.
‘तुलसीदास’ एवं ‘गिरिजाकुमार माथुर’ की काव्य-कला की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
तुलसीदास जी सामाजिक एवं धार्मिक मर्यादाओं के पोषक रहे हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति विशेष के आचरण में जितनी पवित्रता होगी समाज का कल्याण भी उतना ही होगा। इसी तथ्य को उन्होंने ‘विभीषण-रावण संवाद’ के माध्यम से व्यक्त किया है। ये विचार तुलसी ने अवधी भाषा में दोहा एवं चौपाई छन्दों के माध्यम से व्यक्त किए हैं।
गिरिजाकुमार माथुर के गीत छायावादी प्रभाव लिए हुए हैं। उनमें आनन्द, रोमांस और संताप की तरल अनुभूति के साथ लय भी मिलती है। उनके शब्द चयन में तुक-तान और अनुतान की काव्यात्मक झलक मिलती है। वास्तव में वे माँसल रोमांस के वाचिक परम्परा के कवि हैं। आधुनिक कविता के वे श्रेष्ठ कवि हैं।
![]()
विभीषण-रावण संवाद संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या
सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस।
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास॥
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई।
अवसर जानि विभीषन आवा। भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा॥
पुनि सिरू नाइ बैठनिज आसन । बोला बचन पाइ अनुशासन॥
जो कृपाल पूँछिहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहउँ हित ताता॥
जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना॥
सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई।
चौदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोही तिष्टइ नहिं सोई॥
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
सब परिहरि रघुबीरहिभजहुभजहिंजेहि संत ॥1॥
कठिन शब्दार्थ :
सचिव = मंत्री, सलाहकार; बैद = वैद्य (चिकित्सक); गुर = गुरु (शिक्षक); भय = डर के कारण; राज = राज्य; बेगिहीं = शीघ्र; सहाई = सहायक; नाइ = झुकाकर; अनुशासन = आज्ञा; सुजसु = सुन्दर यश; परनारि = पराई स्त्री; लिलार = माथे पर; भुवन = लोक; भूतद्रोही = प्राणियों से शत्रुता रखने वाला।
सन्दर्भ :
यह पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के ‘कल्याण की राह’ के अन्तर्गत ‘विभीषण-रावण-संवाद ‘शीर्षक से लिया गया है। मूलतः यह अंश तुलसीकृत रामचरितमानस’ के ‘सुन्दरकाण्ड’ से लिया गया है।
प्रसंग :
विभीषण अपने भ्राता रावण को नीतिगत बातें बताते हुए कहता है।
व्याख्या :
कविवर तुलसीदास का कथन है कि मंत्री, वैद्य और गुरु यदि भय के कारण प्रिय लगने वाला झूठ बोलते हैं अर्थात् चापलूसीवश सत्य बात न बोलकर मीठी बातें बोलते हैं तो इनसे क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहने का भाव यह है कि यदि मंत्री राज्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन न करके राजा को झूठी खबर या सूचना देता है, यदि वैद्य रोगी की वास्तविक दशा को न बताकर झूठ बोलता है और यदि गुरु भयवश (या स्वार्थवश) धर्म की बात नहीं बोलता है तो इन स्थितियों में क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए।
किन्तु रावण की राजसभा में तो यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय उपयुक्त अवसर समझकर विभीषण वहाँ आ गया। उसने भाई के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरान्त सिर को झुकाकर पुनः प्रणाम करके अपने आसन पर बैठकर और रावण से आज्ञा पाकर इस प्रकार वचन बोला-हे दयामय! आप यदि मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हितकारी बात को कहना चाहता हूँ। हे तात! यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप सुन्दर कीर्ति, सुन्दर बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं तो आप पराई स्त्री के मस्तक को चौथ के चन्द्रमा की भाँति कलंक युक्त मानते हुए उसका परित्याग कर दें।
अर्थात् जिस प्रकार भाद्रपद मास में कृष्णपक्ष की चतुर्थी का चन्द्र दर्शन कलंक का कारण बनता है, उसी भाँति पराई स्त्री को घर में रखना कलंक का कारण है। अतः पराई स्त्री का त्याग करना ही उचित है। अत: तुम श्रीराम की पत्नी सीता को उन्हें वापस लौटा दो। वे चौदह लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके कोई बच नहीं सकता। हे स्वामी! मनुष्य के लिए काम वासना, क्रोध, अहंकार, लिप्सा ये सब नरक के मार्ग हैं अर्थात् इनसे व्यक्ति को नरक का मुँह देखना पड़ता है। अतः इन सबका त्याग करके सीता को राम को सौंपकर उनका भजन करो, जिनका भजन साधु सन्त करते रहते हैं अर्थात् उन श्रीराम की भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है।
विशेष :
- इस पद्यांश में नीति सम्बन्धी वचनों का उपदेश दिया गया है।
- काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि मनुष्य के आन्तरिक शत्रु हैं। मनुष्य अपनी इन्द्रियों पर संयम रखकर इन पर विजय प्राप्त कर सकता है।
- भारतीय पुराणों में ब्रह्माण्ड में स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, आकाश-पाताल आदि चौदह लोक बताए गए हैं।
- भाषा सहज, सरल एवं भावानुकूल हैं।
- चौपाई एवं दोहा छन्द का प्रयोग।
- चौथ के चन्द्र दर्शन से कलंक लगता है। इस जन विश्वास का सटीक वर्णन किया गया है।
तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला॥
ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता॥
गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता।
ताहि बयरू तजि नाइअ माथा। प्रनतारति भंजन रघुनाथा॥
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही। भजन राम बिनु हेतु सनेही॥
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिय रावन॥
बार बार पद लागऊँ विनय करऊँ दससीस।
परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस॥
मुनि पुलकित निज सिष्य सन कहि पठई यह बात।
तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरू तात ॥2॥
कठिन शब्दार्थ :
भूपाला = राजा; भुवनेश्वर = सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के स्वामी; कालहु कर काला = मृत्यु की भी मृत्यु; अज = अजन्मा; अनामय = विकार रहित; अजित = जिससे कोई जीत न सके; अनादि = जिसका आदि नहीं है; मानुष = मनुष्य; जनरंजन = लोगों को प्रसन्न करने वाला; भंजन = नष्ट करने वाला; गो = पृथ्वी; धेनु = गाय; खल ब्राता = दुष्टों के समूह को; रच्छक = रक्षक; बयरू = बैर; नाइअ = झुकाइए; प्रनतारति = शरण में आये हुए के दुःख को; अघ = पाप; त्रय ताप = तीनों तापों को; दससीस = रावण; परहरि = त्यागकर; कोसलाधीस = रामचन्द्रजी; सन = से।
सन्दर्भ :
पूर्ववत्।
प्रसंग :
इस अंश में विभीषण अपने भाई रावण को समझाता है कि वह प्रभु राम को सीता को लौटा दे और प्रभु की शरण में चला जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा।
व्याख्या :
कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हुए कहता है कि हे तात! अर्थात् भाई रावण। काम, क्रोध, मद और लोभ-ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्रीरामचन्द्र जी को भजिए, जिन्हें सन्त पुरुष भजते हैं। हे तात! राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं वे विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई! सुनिए, वे सेवकों को आनन्द देने वाले, दुष्टों के समूह को नष्ट करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अत: आप उनसे बैर त्यागकर उन्हें अपना माथा नवाइए। वे रघुनाथ शरणागत का दुःख नष्ट करने वाले हैं। हे तात! उन प्रभु श्रीराम को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्रीराम को भजिए।
आगे विभीषण समझाता है कि जिसे सम्पूर्ण जगत् से द्रोह (बैर) करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते अर्थात् शरणागत चाहे कितना ही बैरी या पापी क्यों न हो? भगवान श्रीराम उसे अपना लेते हैं। जिनका नाम तीनों तापों (दैविक, दैहिक, भौतिक) का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु (भगवान्) मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण! हृदय में यह बात अच्छी तरह समझ लो।
हे दसशीश! मैं बार-बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्यागकर आप कौशलपति श्रीराम का भजन करिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात तुम्हारे लिए कहला भेजी है। हे तात! सुन्दर अवसर पाकर मैंने तुरन्त यह बात प्रभु अर्थात् आप से कह दी है।
विशेष :
- कवि ने काम, क्रोध, मद एवं मोह को त्यागने का उपदेश दिया है।
- भगवान के निराकार और साकार दोनों रूपों का वर्णन है
- अजित अनादि अनन्ता में अनुप्रास अलंकार है।
- भाषा सहज एवं सरल है।
- शान्त रस।
![]()
माल्यवन्त अति सचिव सयाना। तासु वचन सुनि अति सुख माना॥
तात अनुज तब नीति विभूषन । सो उर धरहु जो कहत विभीषन॥
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दुरिन करहु इहाँ हइ कोऊ॥
माल्यवन्त गृह गयउ बहोरी। कहइ विभीषन पुनि कर जोरी॥
सुमुति कुमति सबके उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥
जहाँ सुमति तहँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना॥
तब उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥
कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥
दोहा : तात चरन गहि मागउँराखहु मोर दुलार।
सीता देहु राम कहुँअहित न होइ तुम्हार ॥3॥
कठिन शब्दार्थ :
सचिव = मन्त्री; सयाना = चतुर; अति = अधिक; अनुज = छोटा भाई; नीति विभूषन = नीतिवान; उर = हृदय में; रिपु = शत्रु; उतकरष = उत्कर्ष, महिमा; सठ = मूर्ख; दुरिन करहुँ = इन्हें दूर कर दो अर्थात् यहाँ से ‘भगा दो; गयउ = चला गया; पुरान = पुराण; निगम = शास्त्र; अस = ऐसा; सुमति = अच्छी बुद्धि; कुमति = दुष्ट बुद्धि; निदाना = परिणाम में; विपरीता = उल्टी; रिपु प्रीता = शत्रु को मित्र; कालराति = कालरात्रि; निसिचर कुल = राक्षस कुल; घनेरी = अधिक; राखहु मोर दुलार = मेरा दुलार रखिए अर्थात् मेरी बात को प्रेमपूर्वक मान लो।
सन्दर्भ :
पूर्ववत्।
प्रसंग :
इस अंश में विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि श्रीराम को उनकी पत्नी लौटा दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
व्याख्या :
कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय विभीषण रावण को नेक सलाह दे रहा था उस समय वहाँ माल्यवन्त नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री बैठा हुआ था। उसने उन (विभीषण) के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा हे तात! (रावण) आपके छोटे भाई बहुत ही नीतिवान हैं। अतः विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए।
इस पर रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई व्यक्ति है जो इन्हें यहाँ से दूर कर दे। यह सुनकर माल्यवन्त तो अपने घर चला गया लेकिन विभीषण पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सभी मनुष्यों के हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की सम्पत्तियाँ आ जाती हैं और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि अर्थात् कुबुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है।
हे तात! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ अर्थात् विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए अर्थात् मेरी बात को स्वीकार कर लीजिए और सीताजी को श्रीराम को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा।
विशेष :
- विभीषण रावण से बार-बार विनती करके सीताजी को लौटाने की प्रार्थना करता है।
- सुमति और कुमति सभी में होती है पर विद्वान लोग सुमति को धारण करते हैं कुमति से दूर रहते हैं।
- अनुप्रास की छटा।
- भाषा सहज एवं सरल है।
- शान्त रस।
सूरज का पहिया संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या
मन में विश्वास का यह सोनचक्र रुके नहीं
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं।
उम्र रहे झलमल
ज्यों सूरज की तश्तरी
डंठल पर विगत के
उगे भविष्य संदली
आँखों में धूप लाल
छाप उन ओठों की
जिसके तन रोओं में
चंदरिमा की कली
छाँह में बरौमियों के चाँद कभी थके नहीं।
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं ॥1॥
कठिन शब्दार्थ :
सोनचक्र = स्वर्णिम पहिया; पियरी = पीली; झलमल = झिलमिलाती रहे, चमकती रहे; सूरज की तश्तरी = सूरज का गोला; विगत = बीते हुए; संदली = चन्दन के समान; चंदरिया = चन्द्रमा।
सन्दर्भ :
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के कल्याण की राह पाठ से गिरिजाकुमार माथुर द्वारा रचित कविता ‘सूरज का पहिया से लिया गया है।
प्रसंग :
इस अंश में कवि संसार के मनुष्यों को सचेत करते हुए कहता है कि तुम विपत्तियों और संकटों में कभी भी घबड़ाना मत और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना।
व्याख्या :
कविवर श्री गिरिजाकुमार माथुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के विश्वास को सदैव मजबूत बनाये रखना चाहिए। वह निरन्तर स्वर्णिम चक्र की भाँति (सूर्य के गोले के समान) निरन्तर गतिशील बना रहना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारे मन में पीली केसर की भाँति जो स्वप्न जन्म ले रहे हैं, वे कभी चुक न जाएँ अर्थात् समाप्त न हो जाएँ। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे मन में जो स्वप्न जन्मे हैं वे सदैव पल्लवित और पुष्पित होते रहें, वे कभी मुरझाएँ नहीं। तुम अपने जीवन में सदैव उसी तरह प्रकाशित होते रहो जिस तरह सूर्य का गोला प्रकाशित होता रहता है।
अतीत के डंठलों पर भविष्य के चन्दनों को उगाओ। कहने का भाव यह है कि अतीत में तुमने अनेकानेक संकट एवं विपत्तियाँ झेली हैं पर अपने भविष्य को तुम चन्दन के समान महकाओ। तुम्हारी आँखों में तुम्हारे विश्वास की रंग-बिरंगी तस्वीर हो। तुम्हारे ओठों पर तुम्हारे स्वप्नों के गीत हों। यदि कभी तुम्हारे जीवन में शाम भी आ जाए अर्थात् निराशा आ जाए तब भी तुम चन्द्रमा के समान अपनी शीतलता बिखेरते रहना। कहने का भाव यह है कि निराशा में भी अपनी आशा का संबल मत छोड़ना। तुम्हारी आँखों की बरौनियों में चन्द्रमा कभी भी थके नहीं अपितु वह निरन्तर गतिशील बना रहे। तुम्हारे जीवन के स्वप्नों की पीली केसर कभी भी मुरझाए नहीं, ऐसा तुम्हें सदैव प्रयत्न करना चाहिए।
विशेष :
- इस कविता में कवि ने सार्थक जीवन जीने का सन्देश दिया है।
- ज्यों सूरज की तश्तरी में उपमा अलंकार।
- भाषा सहज, सरल एवं भावानुकूल है।
![]()
मन में विश्वास
भूमि में ज्यों अंगार रहे
आरई नजरों में
ज्यों अलोप प्यार रहे
पानी में धरा गंध
रुख में बयार रहे
इस विचार-बीज की
फसल बार-बार रहे
मन में संघर्ष फाँस गड़कर भी दुखे नहीं।
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं ॥2॥
कठिन शब्दार्थ :
अंगार = जलता हुआ कोयला; आरई नजरों = प्रेमपूर्ण दृष्टि में; अलोप = प्रकट; धरा = पृथ्वी; गन्ध = सुगन्ध; बयार = वायु; विचार-बीज= विचार रूपी बीज।
सन्दर्भ :
पूर्ववत्।
प्रसंग :
इस अंश में कवि ने जीवन में संचार बनाये रखने तथा निरन्तर आगे बढ़ते रहने का सन्देश दिया है।
व्याख्या :
कविवर माथुर कहते हैं कि हमारे मन में विश्वास की लौ उसी प्रकार प्रज्ज्वलित होती रहनी चाहिए जिस प्रकार पृथ्वी पर जलता हुआ कोयला दिखाई देता है। कहने का भाव यह है कि हमें जीवन में सदैव ऊर्जा का संचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार जल में पृथ्वी की गंध समाई रहती है, जिस प्रकार वायु भी निरन्तर गतिमान रहती है उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य भी निरन्तर गतिमान रहना चाहिए। जिस लक्ष्य को तुमने अपने विचारों में बीज की भाँति बोया है उसे कभी नष्ट नहीं होने देना है। तुम्हें सतत् प्रयत्न करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहना है। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करना है। तुम्हारा विचार बीज कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए अपितु वह बार-बार पल्लवित एवं पुष्पित होते रहना चाहिए। तुम्हें चाहे जीवन में कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े पर इस संघर्ष रूपी काँटे को कभी भी मन में मत चुभाना। इससे अपना मन दुःखी न करना। अपनी पीली केसर जैसी जिन्दगी को कभी भी समाप्त मत होने देना अपितु उसे निरन्तर गतिमान बनाये रखना।
विशेष :
- कवि ने जीवन में सदैव उत्साह भरने की प्रेरणा दी है।
- भूमि में ज्यों अंगार रहे में उपमा अलंकार।
- विचार-बीज में रूपक अलंकार।
- भाषा सहज एवं सरल तथा लाक्षणिक है।
आगम के पंथ मिलें
रंगोली रंग भरे
तिए-सी मंजिल पर
जन भविष्य-दीप पर
धूरी साँझ घिरे
उम्र महागीत बने
सदियों में गूंज भरे।
पाँव में अनीति के मनुष्य कभी झुके नहीं।
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं ॥3॥
कठिन शब्दार्थ :
आगम = शास्त्र, पुराण; भविष्य-दीप= जीवन के भविष्य का दीपक; अनीति = अन्याय; रंगोली = अल्पना।
सन्दर्भ :
पूर्ववत्।
प्रसंग :
कवि का सन्देश है कि हमें निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए और कभी भी अनीति के आगे झुकना नहीं चाहिए।
व्याख्या :
कविवर गिरिजाकुमार माथुर कहते हैं कि हमारे प्राचीन आर्य ग्रन्थ ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएँ और हम अपना जीवन उन्हीं सिद्धान्तों पर जिएँ। हमारे जीवन में सदैव मंगलकारी रंगोलियाँ बनती रहें। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम अपने उज्ज्वल भविष्य के दीप जलाते चलें। हम जीवन में इतना प्रयास करें कि हमारा जीवन स्वयं एक महागीत बन जाए और उसकी गूंज सदियों तक गूंजती रहे। इसके साथ ही हमारे पाँव कभी भी अनीति के सामने झुके नहीं अपितु उन अनीतियों का हमें दृढ़ता से सामना करना चाहिए। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन की पीली केसर कभी समाप्त न होने पाए।
विशेष :
- कवि प्राचीन आगम-निगमों को अपना आदर्श मानता है।
- जीवन में जीवन्तता बनाये रखना ही जीवन का लक्ष्य है।