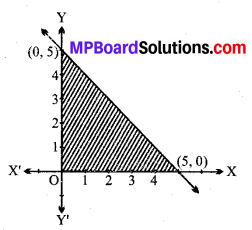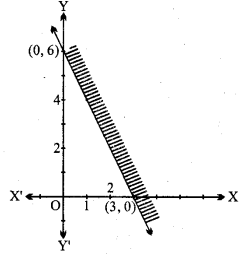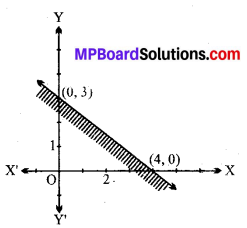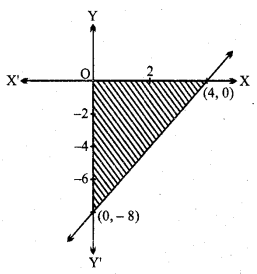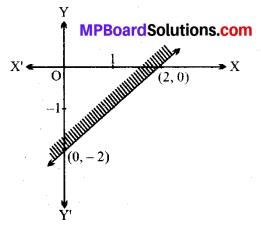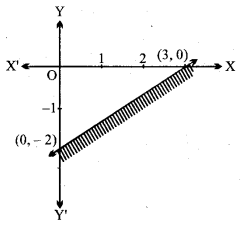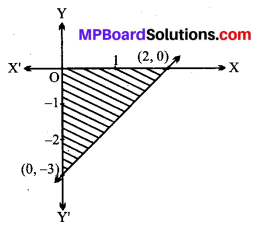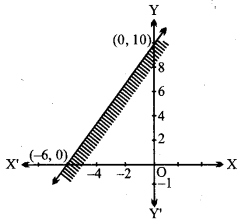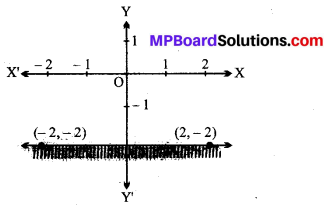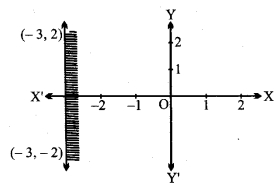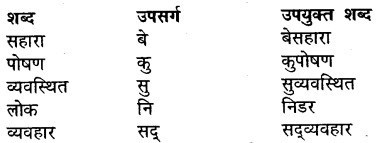MP Board Class 9th Special Hindi अपठित बोध
MP Board Class 9th Special Hindi अपठित गद्यांश
निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
1. मानव जीवन में उत्तरदायित्व का विशेष स्थान है। अवगुणों को दूर करने के लिए एवं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उत्तरदायित्व आ जाने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। उदाहरण के लिए, बुरी आदतों वाले लोग, शिक्षक जैसे पद को प्राप्त कर अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार उद्दण्ड नवयुवक भी गृहस्थी का भार आ जाने पर विचारशील बन जाते हैं।
प्रश्न
1. उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त (सटीक) शीर्षक चुनिए।
2. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
3. लोग अपनी बुरी आदतों को कब छोड़ देते हैं?
4. विलोम शब्द बताइए-सफलता, आवश्यक।
5. ‘उत्तरदायित्व’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. ‘उत्तरदायित्व’।
2. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक हैं।
3. लोग अपनी बुरी आदतों को शिक्षक जैसे पद को प्राप्त करके छोड़ देते हैं।
4. असफलता, अनावश्यक।
5. ‘उत्तरदायित्व’ का निर्वाह करने पर मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकता है।
![]()
2. राष्ट्रीय एकता प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए नितान्त आवश्यक है। जब भी धार्मिक या जातीय आधार पर राष्ट्र से अलग होने की कोशिश होती है, हमारी राष्ट्रीय एकता के खण्डित होने का खतरा बढ़ जाता है। यह एक सुनिश्चित सत्य है कि राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करने में वहाँ निवास करने वाले जन एक अनिवार्य तत्व होते हैं। भावात्मक स्तर पर स्नेह सम्बन्ध सहिष्णुता, पारस्परिक सहयोग एवं उदार मनोवृत्ति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति होती है। राष्ट्र को केवल भूखण्ड मानकर उसके प्रति अपने कर्तव्यों से उदासीन होने वाले जन राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में कदापि सहायक नहीं हो सकते। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता को व्यवहार में अवतरित करके ही राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
प्रश्न
1. उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त (सटीक) शीर्षक लिखिए।
2. उपर्युक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
3. राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब उत्पन्न होता है?
4. विलोम शब्द बताइए-एकता, उदार।
5. ‘उन्नति’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. उपर्युक्त शीर्षक–’राष्ट्रीय एकता’।
2. किसी देश की स्वतन्त्रता एकता के द्वारा ही स्थायी रह सकती है। राष्ट्रीय एकता का मूलाधार वहाँ निवास करने वाले लोगों के उत्तम संस्कार एवं श्रेष्ठ विचार हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक मानव को सहगामी बनाना चाहिए।
3. राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उस समय उत्पन्न होता है, जब धर्म एवं जाति को माध्यम बनाकर राष्ट्र से पृथक् होने की कोशिश की जाती है।
4. अनेकता, अनुदार।
5. देश की उन्नति’ प्रत्येक नागरिक के चारित्रिक गुणों के विकास पर निर्भर हैं।
3. कविता ही मनुष्य को हृदय के स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। जहाँ जगत् की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति है। इस अनुभूति के आभास से हमारे मनोविकार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।
प्रश्न
1. उपर्युक्त गद्यांश का उचित (सटीक) शीर्षक लिखिए।
2. कविता मनुष्य के लिए क्या काम करती है?
3. उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।
4. विलोम शब्द बताइए-स्वार्थ, शेष।
5. ‘रागात्मक’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. कविता का स्वरूप।
2. कविता ही मनुष्य को हृदय के स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर ले जाती है।
3. कविता मनुष्य को स्वार्थ से अलग करती है। उसकी संकुचित व संकीर्ण मानसिकता को व्यापक रूप प्रदान करती है। मनुष्य हृदय में कविता से संवेदना का भाव जगता है। वह संसार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसी गुण के विकास से वह दूसरों की अनुभूति को अपनी अनुभूति मान लेता है।
4. परार्थ, अशेष।
5. सृष्टि के प्रति हमारा रागात्मक सम्बन्ध कविता के द्वारा स्थापित होता है।
4. समाजवाद एक सुन्दर शब्द है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाजवाद में समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा और न कोई ऊँचा। किसी आदमी के शरीर में सिर इसलिए ऊँचा नहीं है कि वह सबसे ऊपर है और पाँव के तलवे इसलिए नीचे नहीं हैं कि वे जमीन को छूते हैं। जिस तरह मनुष्य के शरीर के सारे अंग बराबर हैं उसी प्रकार समाज में सभी मनुष्य समान हैं; यही समाजवाद है।
प्रश्न.
1. उपर्युक्त गद्यांश का उचित (सटीक) शीर्षक दीजिए।
2. उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।
3. समाजवाद में महत्त्व की बात क्या है?
4. विलोम शब्द बताइए-छूते हैं, नीचा।
5. ‘सदस्य’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. शीर्षक-‘समाजवाद’।
2. समाजवाद की व्यवस्था आदमी के शरीर की भाँति है। जहाँ समाज के सारे सदस्य एक बराबर होते हैं न कोई नीचा और न कोई ऊँचा।
3. समाजवाद में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं।
4. अछूते हैं, ऊँचा।
5. घर के सदस्य मिलकर अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं।
MP Board Class 9th Special Hindi अपठित पद्यांश
निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सावधानीपूर्वक दीजिए-
1. निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल॥
इक भाषा इक जीव, इक मीत सब घर के लोग।
तब बनत है सबन सौं, मिटत मूढ़ता सोग॥
प्रश्न
1. उपर्युक्त पद्यांश का उचित (सटीक) शीर्षक लिखिए।
2. उपर्युक्त पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए।
3. कविकेअनुसार मूढ़ता और शोक किस प्रकार मिटता है?
4. शब्दार्थ बताइए-निज, सूल।
5. ‘ज्ञान’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. शीर्षक-‘राष्ट्रभाषा की उन्नति’।
2. भावार्थ-अपनी राष्ट्र भाषा की उन्नति और विकास से ही सभी प्रकार की उन्नति सम्भव है। अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके ही अपने हृदय की बात को, व्यथा को बता सकते हैं। जब सम्पूर्ण राष्ट्र के लोग एक भाषा, एक ही तरह की जीवन-शैली एवं समान विचारधारा अपनायेंगे, तो अवश्य ही उनकी मूर्खता एवं शोक (कष्ट) दूर हो सकेंगे।
3. कवि के अनुसार जब सभी लोग एक ही भाषा एवं एक जैसी जीवन शैली एवं विचार अपनायेंगे, तभी उनकी मूढ़ता एवं शोक मिट सकेंगे।
4. अपना, कष्ट।
5. ‘ज्ञान’ से मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है।
![]()
2. सावधान मनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार,
तो इसे दो फेंक तजकर मोह, स्मृति के सार।
हो चुका है सिद्ध ! है तू शिशु अभी अज्ञान;
फूल काँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान।
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार,
काट लेगा अंग, तीखी है, बड़ी ये धार।
प्रश्न
1. उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त (सटीक) शीर्षक लिखिए।
2. उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
3. ‘फूल और काँटों’ से कवि का क्या तात्पर्य है?
4. विलोम शब्द बताइए-स्मृति, अज्ञान।
5. ‘धार’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. उपयुक्त शीर्षक ‘विज्ञान से सचेत’।
2. कवि का आशय यह है कि मनुष्य को विज्ञान से सावधान रहना चाहिए। इसका प्रयोग अज्ञानता से नहीं कीजिए। मनुष्य ने अभी विज्ञान से होने वाली हानि और लाभ की भी जानकारी नहीं ली है। अतः कहीं ऐसा न हो कि अज्ञानता के कारण यह विज्ञान मनुष्य को ही हानि न पहुँचा दे।
3. ‘फूल और काँटों’ से कवि का तात्पर्य है-लाभ और हानि।
4. विस्मृति, ज्ञान।
5. तलवार की धार तेज होती है।
3. बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से,
मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से;
रानी से भी अधिक हमें अब, यह समाधि है प्यारी,
यहाँ निहित है स्वतन्त्रता की, आशा की चिनगारी॥
प्रश्न
1. उपर्युक्त कविता का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
2. पद्यांश का आशय लिखिए।
3. वीर का मान कब बढ़ जाता है?
4. विलोम शब्द बताइए-वीर, स्वतन्त्रता।
5. ‘निहित’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. ‘स्वतन्त्रता’ इस पद्यांश का उचित शीर्षक है।
2. जब युद्ध में संघर्षरत वीर स्वयं को आजादी को प्राप्त करने के महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहीद कर देता है, तो उसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तीव्र ज्वाला में जलकर स्वर्ण की भस्म तैयार होती है। वह भस्म निश्चय ही उस धातु की अपेक्षा कई गुना लाभ देने वाली होगी। सभी लोग उसको सम्मान देते हैं।
3. वीर का मान उस समय बढ़ जाता है, जब वह स्वयं को राष्ट्र की स्वतन्त्रता के बचाव में बलिदान कर देता है।
4. कायर, परतन्त्रता।
5. बालक में शिक्षा के द्वारा उसके निहित गुणों को उभारना होता है।
![]()
4. लाख पक्षी सौ हिरन दल, चाँद के कितने किरण दल,
झूमते वन-फूल फलियाँ, खिल रहीं अज्ञात कलियाँ,
हरित दूर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय,
सतपुड़ा के घने जंगल।
प्रश्न
1. उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।
2. कवि ने इस पद्यांश में कहाँ का वर्णन किया है?
3. पद्यांश का आशय लिखिए।
4. विलोम शब्द बताइए-अज्ञात, पावन।
5. ‘घने’ शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
1. शीर्षक-‘सतपुड़ा के घने जंगल’।
2. कवि ने इस पद्यांश में सतपुड़ा के घने जंगलों का वर्णन किया है।
3. कवि का आशय है कि सतपुड़ा के घने जंगलों में लाखों पक्षी और हिरणों के समूह विचरण करते सुन्दर लगते हैं। चन्द्रमा की चाँदनी अपनी छटा बिखेरती रहती है। वहाँ वन के फूल और फलियाँ निरन्तर विकसित होते रहते हैं जिनकी पूर्ण जानकारी हमें नहीं है। कहीं-कहीं हरी-भरी दूब घास अपने लाल-लाल किसलयों से युक्त विकास पा रहे हैं। वे वातावरण को पूर्ण पवित्रता दे रहे हैं।
4. ज्ञात, अपावन।
5. घने वन में असंख्य पशु-पक्षी रहते हैं।