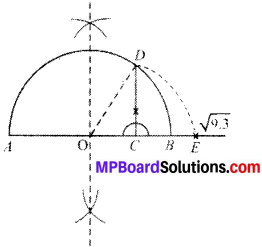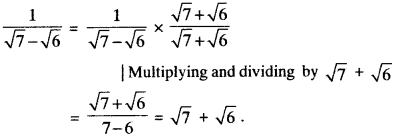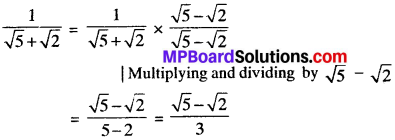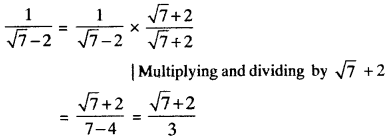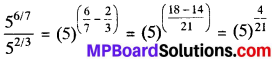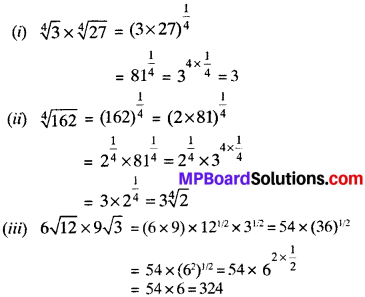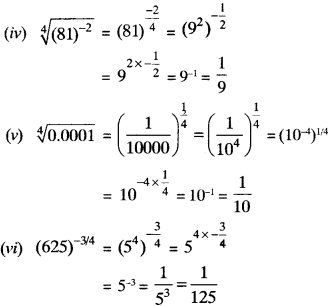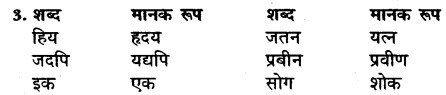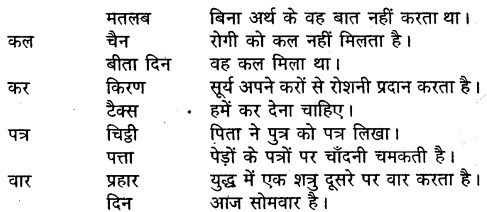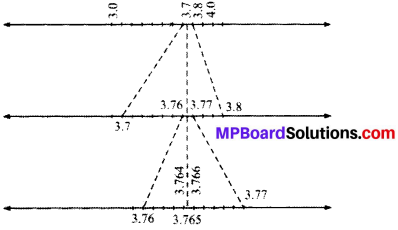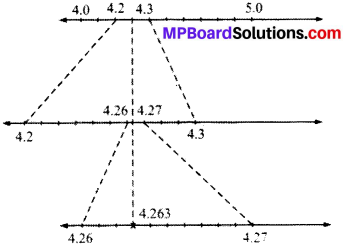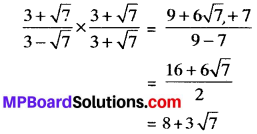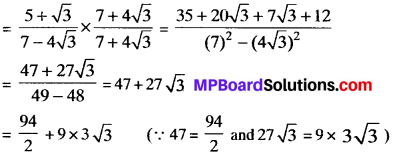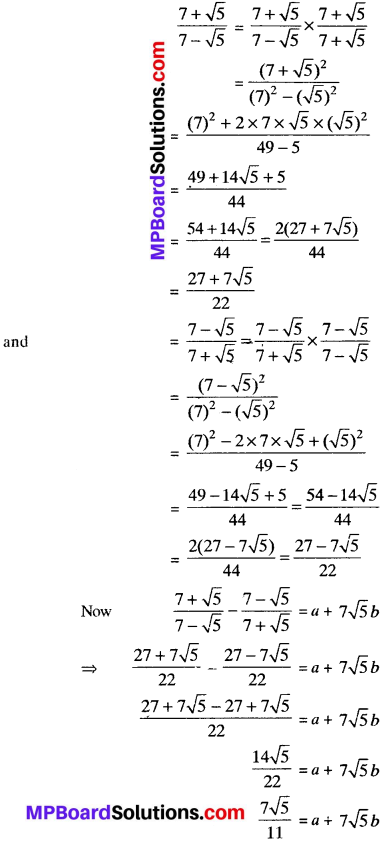MP Board Class 9th Hindi Vasanti Solutions Chapter 11 जागरण गीत (सोहनलाल द्विवेदी)
जागरण गीत अभ्यास-प्रश्न
जागरण गीत लघूत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
कवि गीत गाकर ही लोगों को क्यों जगाना चाहता है?
उत्तर
कवि गीत गाकर ही लोगों को जगाना चाहता है। यह इसलिए कि साधारण रूप से कही गई बातों की अपेक्षा गीत के माध्यम से कही बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं।
प्रश्न 2.
इस गीत में किस रास्ते को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है?
उत्तर
इस गीत में उदयाचल को सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताया गया है।
![]()
प्रश्न 3.
कवि किस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए आतुर है?
उत्तर
कवि प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए आतुर है।
प्रश्न 4.
संकीर्णताएँ तोड़ने के लिए कवि क्या करना चाहता है?
उत्तर
संकीर्णताएँ तोड़ने के लिए कवि सोए हुए दृढ़ भावों को जगाना चाहता है।
जागरण गीत दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
कवि आकाश में उड़ने के लिए क्यों रोक रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
कवि आकाश में उड़ने के लिए रोक रहा है। यह इसलिए कि इससे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। फलस्वरूप जीवन दुखद और निरर्थक बना रहता है।
प्रश्न 2.
शूल को फूल बनाने से कवि का क्या आशय है?
उत्तर
शूल को फूल बनाने से कवि का आशय है-जीवन में आने वाली कठिनाइयों, रुकावटों और कष्टों को अपनी क्षमता, शक्ति आर बुद्धिबल से दूर करके जीवन को हर प्रकार से सुखद और सुन्दर बना लेना। इसके द्वारा कवि ने आलसी और निराश लोगों को प्रेरित और उत्साहित करना चाहा है।
![]()
प्रश्न 3.
‘अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूँगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ।’ उपरोक्त पंक्तियों का भावार्य लिखिए।
उत्तर
अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ।’ उपरोक्त पंक्तियों के द्वारा कवि ने यह भाव दर्शाना चाहा है कि गहरी नींद में पड़े रहना, जीवन की सच्चाई को नकारना है। इस प्रकार का जीवन डूबते हुए सूरज के समान है, जिसमें न कोई आशा, विश्वास, आकर्षण, समुल्लास आदि जीवन-स्वरूप दिखाई देते हैं। इस प्रकार का जीवन न स्वयं के लिए अपितु दूसरे के लिए भी दुखद और कष्टकर होता है। इसलिए इस प्रकार के जीवन का परित्याग करके अरुण उदयाचल अर्थात् प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए हर प्रकार से कदम बढ़ाना चाहिए।
प्रश्न 4.
विपथ होकर मुड़ने का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
विपथ होकर मुड़ने का आशय है-सन्मार्ग से हटकर कुमार्ग पर चलना। दूसरे शब्दों में अच्छाई और सुन्दरता को छोड़कर बुराई और कुरूपता को अपनाना।
जागरण गीत भाषा-अध्ययन/काव्य-सौन्दर्य
प्रश्न 1.
निम्नलिखित शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं उन्हें दूर कर पुनः लिखिए।
अरूण, सीस, सूल, मंझदार, श्रृंखलाएँ, पातवार, पृगति, संकीणताएँ, विपथ, झनझनाये।
उत्तर
अशुद्धियाँ – शुद्धियाँ
अरूण – अरुण
शीस – शीश
सूल – शूल
मंझदार – मैंनधार
श्रृंखलाएँ – श्रृंखलाएँ
पातवार – पतवार
पृगति – प्रगति
संकीणताएँ – संकीर्णताएँ
विपथ – बिपथ
झनझनाये – झनझनाए।
प्रश्न 2.
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर पुनः वाक्य लिखिए
1. अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा।
2. फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ।
3. विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा।
4. मैं किनारे पर तुम्हें बकने न दूंगा।
5. सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ।
उत्तर
- अब तुम्हें आसमान में उड़ने न दूंगा।
- पुष्प मैं उसको बनाने आ रहा हूँ।
- कुपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा।
- मैं तट पर तुम्हें थकने न दूँगा।
- समुद्र बन तुमको उठाने आ रहा हूँ।
प्रश्न 3.
निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और पाठ में आए शब्दों में से स्वर मैत्री समझकर लिखिए
अस्ताचल – उदयाचल
साधना – ……………..
मैंनदार – ………………..
उठाए – ……………….
गति – ………………..
शूल – ……………
उत्तर
अस्ताचल – उदयाचल
साधना – कल्पना
मँझदार – पतवार
उठाए – झनझजाए
गति – गति
शूल – फूल
जागरण गीत योग्यता-विस्तार
प्रश्न 1.
जीवन में प्रगति तभी सम्भव है जब हम निराशा के क्षणों में तथा विरोधी परिस्थितियों में संघर्षरत रहकर आशावादी दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ें। इस सन्दर्भ की अन्य कविताएँ संकलित कीजिए तवा विभिन्न अवसरों पर अपने मित्रों/साथियों को सुलेख में लिखकर भेंट करें।
प्रश्न 2.
कक्षा में एक डिब्बा रखिए। अपने साथियों के किस गुण से किस परिस्थिति से आप प्रभावित हुए एक कागज पर लिखकर डिब्बे में डालिए। कुछ दिनों के उपरांत अपने शिक्षक एवं कक्षा के सम्मुख उन्हें खोलकर सबको सुनाएँ।
उत्तर
उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से हल करें।
जागरण गीत परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
लघूत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
गहरी नींद में सोने वाले अब सो न सकेंगे। क्यों?
उत्तर
गहरी नींद में सोने वाले अब सो न सकेंगे। यह इसलिए कि कवि उन्हें गीत गाकर जगाने आ रहा है।
प्रश्न 2.
कवि अस्ताचल जाने के बजाय कहा जाने की बात कह रहा है? उत्तर-कवि अस्ताचल जाने के बजाय उदयाचल जाने की बात कह रहा है। प्रश्न 3. कवि के अनुसार क्या दुख-सुख है?
उत्तर
कवि के अनुसार नींद में सपने संजोना दुख है और इससे हटकर परिश्रम पूर्वक जीवन जीना सुख है।
![]()
प्रश्न 4.
मैंनधार से किनारे पर आने के लिए कवि ने क्या कहा है?
उत्तर
मँझधार से किनारे पर आने के लिए कवि ने कहा है कि मैंझधार में पड़ने पर घबड़ाना नहीं चाहिए। हिम्मत करके विश्वासपूर्वक हाथ में पतवार लेकर किनारे की ओर आने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
जागरण गीत दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
कवि गीत किसके लिए गा रहा है?
उत्तर
कवि गहरी नींद में सोने वालों, अतल अस्ताचल की ओर जाने वालों, कल्पना के पंख लगाकर आकाश में उड़ने वालों, जीवन को काँटा समझने वालों, जीवन के मँझधार में पड़कर घबड़ाने और थकने वालों, मन में तुच्छ विचारों को रखने वालों और विपथ होकर जीवन की सच्चाई को नकारने वालों के लिए गीत गा रहा है।
प्रश्न 2.
‘आ रहा हूँ। ऐसा कवि ने बार-बार क्यों कहा है?
उत्तर
‘आ रहा हूँ।’ ऐसा कवि ने बार-बार कहा है। यह इसलिए कि इसके द्वारा वह अपना जागरण सन्देश देना चाहा है। उसने अपना यह जागरण सन्देश उन लोगों को ही देना चाहा है, जो जीवन की सच्चाई को नकारते रहे हैं और संकीर्ण मनोवृत्तियों जैसे-आलस्य, निराशा आदि को स्वीकारते रहे हैं। कवि इस प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्तियों को त्यागकर कर्मरत होते हुए जीवन की वास्तविकता को स्वीकारने के लिए ही बार-बार ‘आ रहा हूँ। कहकर आत्मीयता प्रकट करना चाहता है।
![]()
प्रश्न 3.
‘जागरण गीत’ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
श्री सोहनलाल द्विवेदी-विरचित कविता ‘जागरण गीत’ एक प्रेरक कविता है। इस गीत के द्वारा द्विवेदी जी ने बड़े ही नपे-तुले शब्दों में जीवन की सार्थकता को बतलाने का प्रयास किया है। द्विवेदी जी इस जागरण गीत के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का चित्रण किया है। उन्होंने यह बतलाना चाहा है कि जीवन में आलस्य, निराशा तथा संकीर्ण मनोवृत्ति को नकारते हुए मनोवृत्ति कर्मरत जीवन को ही प्रगति का मूलमंत्र बताया है। इस प्रकार उन्होंने पुराने मिथक तोड़ते हुए नव-जीवन के संचार का सन्देश इस गीत माध्यम से दिया है।
जागरण गीत कवि-परिचय
प्रश्न
श्री सोहनलाल द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनके साहित्य के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर
जीवन-परचिय-श्री सोहनलाल द्विवेदी का राष्ट्रीय विचारधारा के कवियों में प्रमुख स्थान है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का अधिक स्वर सुनाई पड़ता है। उनका जन्म सन् 1905 ई. में हुआ था। उन्होंने छोटी-सी आयु में ही काव्य-रचना आरम्भ किया, जो क्रमशः देश-प्रेम और भक्ति के स्वर से गुंजित होता गया। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रवाह है, तो गाँधीवादी चिन्तन और दृष्टिकोण भी है।
रचनाएँ-द्विवेजी जी की निम्नलिखत-रचनाएँ हैं-भैरवी-पूजा, ‘गीत’, ‘सेवाग्राम’, ‘दूध बतासा’, ‘चेतना’,’बाल भारती’ आदि।
भाषा-शैली-द्विवेदी जी की भाषा सहज और ऐसे प्रचलित शब्दों की है, जिसमें विविधता और अनेकरूपता है। तत्सम शब्दों की अधिकता है। जिसकी सहजता के लिए तभव और देशज शब्द बड़े ही उपयुक्त और सटीक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। कहीं-कहीं मुहावरों-कहावतों को प्रयुक्त किया गया है। उनसे भाषा में और सजीवता आ गई है। बोधगम्यता और प्रवाहमयता उनकी शैली की पहली विशेषता है।
महत्त्व-द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के प्रबल समर्थक थे चूँकि गाँधी की विचारधारा से वे पूरी तरह प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने उसका न केवल समर्थन किया, अपितु उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से जन-जन तक प्रेरित भी किया। गाँधीवादी विचारधारा में आस्था रखने के कारण उनकी रचनाओं में प्रेम, अहिंसा और समता के भाव दिखाई देते हैं। इस प्रकार वे अपने विशिष्ट योगदानों के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे।
जागरण गीत कविता का सारांश
प्रश्न
सोहन लात द्विवेदी विरचित कविता ‘जागरण गीत’ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर
श्री सोहनलाल द्विवेदी-विरचित कविता ‘जागरण गीत’ एक भाववर्द्धक और सन्देशवाहक कविता है। इसमें कवि ने यथार्थ जीवन जीने का सन्देश दिया है। इस कविता का सारांश इस प्रकार है कवि गहरी नींद में सोने वालों से कह रहा है कि वह गीत गाकर उसे जगाने के लिए आ रहा है। वह अब नींद की गहराई से ऊपर निकालकर उसे आकर्षक उदयाचल की तरह उत्साह प्रदान करने का जागरण गीत गा रहा है। कवि गहरी नींद में सोने वाले को फटकारते हुए कह रहा है कि वह आज तक नींद में पड़े-पड़े मीठी-मीठी कल्पना का उड़ान भरता रहा है। परिश्रम करने से कतराता रहा है।
![]()
लेकिन वह ऐसा नहीं कर पायेगा। ऐसा इसलिए कि वह अपने जागरण गीत से उसे यथार्थ जमीन पर ला देगा। उसमें यह चेतना ला देगा कि नींद में सपने देखना सुखदायक नहीं है। उसके दुःखों को सुखों में वह अपने जागरण गीत से फूल में बदल देगा। गहरी नींद में सोने वाले को कवि की सीख है कि उसे जीवन के दुखों के मझधार में पड़ने पर घबड़ाना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कि वह अपने जागरण गीत से उसे पार लगा देगा। इसलिए उसे अपने मन में उठने वाली छोटी-छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपने जागरण गीत से उसकी हीनता को समाप्त कर देगा। यह सोच-समझकर अपने जीवन-पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते जाओ। वह अपने जागरण गीत से उसे उसके प्रगति के पथ से पीछे नहीं मुड़ने देगा।
जागरण गीत संदर्भ-प्रसंग सहित व्याख्या
पद की सप्रसंग व्याख्या, काव्य-सौन्दर्य व विषय-वस्तु पर आधारित प्रश्नोत्तर
1. अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे,
गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ।
अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा,
अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ॥
कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम,
साधना से सिहरकर मुड़ते रहे तुम।
अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूँगा,
आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ॥
शब्दार्च-अतल-गहराई। अस्ताचल-पश्चिम का वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होना माना जाता है। उदयाचल-पूर्व का वह कल्पित पर्वत जहाँ से सूर्य उदित होता है।
प्रसंग-प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘वासन्ती’ हिन्दी सामान्य में संकलित तथा श्री सोहनलाल द्विवेदी विरचित कविता ‘जागरण गीत’ से है। इसमें कवि ने आलसी मनुष्यों को सावधान करते हुए कहा है कि
व्याख्या-अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा। मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अस्ताचल की गहराई अर्थात् जीवन की बर्बादी की ओर तुम्हें जाने से रोकने के लिए मैं आकर्षक उदयाचल को सजाने के लिए अर्थात् तुम्हारे जीवन को आनन्दित बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें अपने-आपके विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि तुम आज तक कल्पना की ऊँची उड़ान उड़ते रहे हो। परिश्रम से मुँह मोड़ते रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो मैं आकाश की उड़ान से नीचे धरती पर लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हैं। दूसरे शब्दों में तम्हें जीवन की वास्तविकता बतलाने-समझाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
विशेष-
- कवि का जागरण-सन्देश भाववर्द्धक है।
- शब्द-चयन लाक्षणिक है।
- तत्सम शब्दों एवं तदभव शब्दों के प्रयोग सटीक हैं।
- शैली उपदेशात्मक-भावात्मक है।
- वीर रस का संचार है।
![]()
1. पद्यांश पर आधारित काव्य-सौन्दर्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
प्रश्न
(i) प्रस्तुत पद्यांश का काव्य-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।
(ii) प्रस्तुत पयांश का भाव-सौन्दर्य लिखिए।
उत्तर
(i) प्रस्तुत पद्यांश का काव्य-सौन्दर्य काव्यांग के स्वरूपों से पष्ट है। अनप्रास अलंकार की छटा (गीत गाकार व अतल अस्ताचल) इस पद्यांश में जहाँ है, वहीं मुहावरेदार शैली (गहरी नींद में सोना, आकाश में उड़ना और धरती पर बसाना) का प्रयोग आकर्षक है। वीर रस से यह अंश अधिक गतिशील होकर ओजपूर्ण बन गया है।
(ii) प्रस्तुत पद्यांश का भाव-सौन्दर्य सरस और सहज शब्दों का है गहरी नींद में गीत गाकर जगाने का भाव न केवल अनूठा है अपित आत्मीयता से परिपूर्ण है।
गहरी नींद की सच्चाई को विश्वसनीयता के साथ बतलाने का ढंग रोचक होने के । साथ प्रेरक भी है। इससे कथन की सफलता को नकारा नहीं जा सकता है।
2. पद्यांश पर आधारित विषय-वस्त से सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
प्रश्न
(i) कवि गीत गाकर किसे जगाना चाहता है?
(ii) आकाश में उड़ने के लिए कवि क्यों मना करता है?
उत्तर
(i) कवि गीत गाकर गहरी नींद में सोने वाले को जगाना चाहता है।
(ii) आकाश में उड़ने के लिए कवि मना करता है। यह इसलिए कि इससे जीवन की निरर्थकता सिद्ध होती है।
2. सुख नहीं यह, नींद में सपने संजोना,
दुख नहीं यह, शीश पर गुरू भार ढोना।
शूल तुम जिसको समझते वे अभी तक,
फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ।
देखकर मँझधार को घबरा न जाना,
हाथ ले पतवार को घबरा न जाना।
मैं किनारे पर तुम्हें चकने न दूंगा,
पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ।
शब्दार्थ-गुरूभार-भारीभार। शूल-काँटा (कठिनाई)। मझधार-बीच धारा।
प्रसंग-पूर्ववत् । इस पद्यांश में कवि ने कायर और आलसी मनुष्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि
व्याख्या-हे आलसी, कायर मनुष्य! तुम्हें यह बात गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना किसी प्रकार से सुखद नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह हर प्रकार से दुखद और हानिकर ही होगा। इस प्रकार दुःखद होगा कि यह सिर का एक बहुत बड़ा बोझ बन जायेगा। उसे ढो पाना निश्चय ही असम्भव होगा। अब तक तुमने जिसे फूल अर्थात् जीवन की कठिनता समझते आ रहे हो। उसे ही मैं फूल बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
कवि का पुनः गहरी नींद में सोने वाले अर्थात् जीवन-संघर्ष से भागने वाले मनुष्य को समुत्साहित करते हुए कहना है कि तुम स्वयं को जीवन-सागर के मँझधार में पाकर घबड़ाओ नहीं, अपितु धैर्य और हिम्मत से काम लो। जीवन-सागर के मँझधार से निकलकर किनारे पर आने के लिए तुम धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में संभाल लो। इस प्रकार जब तुम साहस करोगे तो मैं तुम्हें किनारे पर आने तक उत्साहित करते हुए किसी प्रकार से निराश नहीं होने दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन-सागर से पार लगाने के लिए ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
विशेष-
- वीर रस का प्रवाह है।
- तुकान्त शब्दावली है।
- शैली उपदेशात्मक है।
- ‘नींद में सपने संजोना’, ‘फूल बनाना’, हाथ में पतवार लेना और पार लगाना मुहावरों के सटीक और सार्थक प्रयोग हैं।
1. पद्यांश पर आधारित काव्य-सौन्दर्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
प्रश्न
(i) प्रस्तुत पयांश का काव्य-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।
(ii) प्रस्तुत पयांश का भाक्-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
(i) प्रस्तुत पद्यांश को काव्य:विधान-स्वरूप शब्द-भाव-योजना से निखारने का प्रयास प्रशंसनीय कहा जा सकता है। ‘घबरा न जाना’ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से अलंकृत यह पद्यांश कई मुहावरों के एकजुट आने से अधिक भावपूर्ण होकर सार्थकता में बदल गया है।
(ii) प्रस्तुत पद्यांश की भाव-योजना अपनी प्रभावमयता के फलस्वरूप रोचक और आकर्षक है। निराश और जीवन-संघर्ष के सामने घुटना टेकने वालों को सत्प्रेरित करने के विविध प्रयास प्रभावशाली रूप में हैं।
![]()
2. पद्यांश पर आधारित विषय-वस्त से सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
प्रश्न
(i) नींद में सपने संजोना क्यों नहीं सुखद है?
(ii) मँझधार में पड़ने पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए?
उत्तर-
(i) नींद में सपने संजोना सुखद नहीं है। यह इसलिए कि इससे दुखों का बोझ कम न होकर बहुत भारी हो जाता है। फिर उसे ढोना असम्भव-सा हो जाता है।
(ii) मँझधार में पड़ने पर घबड़ाना नहीं चाहिए। हाथ में पतवार लेकर किनारे पर आने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए।
3. तोड़ दो मन में कसी सब शृंखलाएँ
तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएँ।
बिन्दु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा
सिन्धु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ॥
तुम उठो, धरती उठे, नभ शिर उठाए,
तुम चलो गति में नई गति झनझनाए।
विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा,
प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ॥
शब्दार्व-संकीर्णताएँ-तुच्छ विचार । श्रृंखलाएँ-कड़ियाँ। नभ-आकाश । शिर-मस्तक, सिर। विपथ-बुरा रास्ता। प्रगति-उन्नति।
प्रसंग-पूर्ववत् । इसमें कवि ने आलसी और निराश व्यक्ति को समुत्साहित करते हुए कहा है कि
व्याख्या-तुम अपने मन को हीन करने वाली विचारों की कड़ियों को खण्ड-खण्ड कर डालो। इसी प्रकार तुम अपने अन्दर के तुच्छ विचारों और हीन भावों का परित्याग कर दो। तुम्हें स्वयं को कम न समझते हुए समुद्र की तरह विशाल और असीमित शक्ति से भरपूर समझना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो मैं तुम्हें ऐसा समझने के भावों को तुम्हारे अन्दर से जगाऊँगा।
इस प्रकार तुम्हें एक बिन्दु के समान जीवन जीने की स्थिति में नहीं रहने देगा। मैं तो तुम्हें समुद्र की तरह जीने देने के लिए तुम्हारे अन्दर सोई हुई भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ। कवि का पुनः जीवन में हारे हुए और निराश व्यक्ति को समुत्साहित करते हुए कहना है कि तुम अब अपनी गहरी नींद से जग जाओ। तुम्हारी जागृति और चेतना से इस संसार में जागृति और चेतना आ जाएगी। सारा आसमान अपना मस्तक ऊंचा कर लेगा। तुम्हारे गतिशील होने से सब ओर गतिशीलता आ जाएगी। तुम्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे जीवन में हारने नहीं दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ।
विशेष-
- भाषा में ओज और गति है।
- मुहावरों के प्रयोग सटीक हैं।
- शब्द-चयन प्रचलित रूप में है।
- वीर रस का प्रवाह है।
![]()
1. पद्यांश पर आधारित काव्य-सौन्दर्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
प्रश्न
(i) उपर्युक्त पयांश के काव्य-सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए।
(ii) उपर्युक्त पद्यांश के भाव-सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
(i) उपर्युक्त पद्यांश का काव्य-स्वरूप प्रचलित तत्सम शब्दावली से परिपुष्ट है। उसे रोचक और आकर्षक बनाने के लिए तुकान्त शब्दावली की योजना ने लय
और संगीत को प्रस्तुत करके भाववर्द्धक बना दिया है। वीर रस के प्रवाह-संचार से यह पद्यांश प्रेरक रूप में है।
(ii) उपर्युक्त पद्यांश का भाव-सौन्दर्य वीरता के भावों से प्रेरक रूप में है। निराश मनों को वीर रस से संचारित करने का प्रयास प्रशंसनीय है। भाव और अर्थ का सुन्दर मेल है।
2. पद्यांश पर आधारित विषय-वस्त से सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
प्रश्न
(i) ‘शृंखलाओं’ से कवि का क्या आशय है?
(ii) ‘विपव’ से कवि का क्या तात्पर्य है?
उत्तर
(i) शृंखलाओं से कवि का आशय है हीन भावनाएँ।
(ii) ‘विपथ’ से कवि का तात्पर्य है-कुपथ। सन्मार्ग को छोड़कर दुखद रास्ते पर चलना।