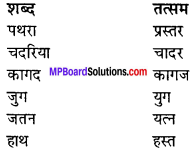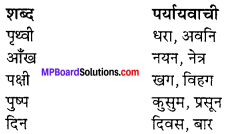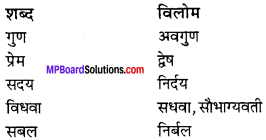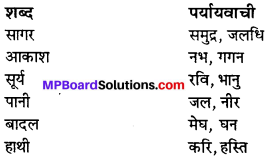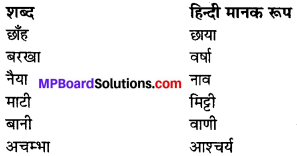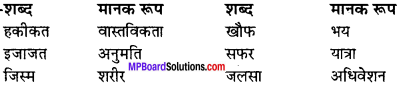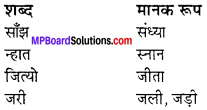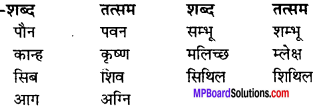MP Board Class 11th Hindi Swati Solutions गद्य Chapter 2 शिरीष के फूल
शिरीष के फूल अभ्यास
शिरीष के फूल अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
शिरीष किस ऋतु में फूलता है?
उत्तर:
शिरीष जेठ मास की तपती धूप में फलता-फूलता है।
प्रश्न 2.
शिरीष की तुलना किससे की गई है?
उत्तर:
शिरीष की तुलना अद्भुत अवधूत से की गई है।
प्रश्न 3.
शिरीष अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? (2017)
उत्तर:
शिरीष अपना पोषण वायुमण्डल से रस खींचकर प्राप्त करता है।
![]()
शिरीष के फूल लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
“शिरीष निर्धात फलता रहता है।” लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? (2014)
उत्तर:
शिरीष जेठ मासं की गर्मी में तो फलता-फूलता ही है बसन्त के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ में मस्ती से भरा रहता है। यदि इच्छा हुई एवं मन रम गया तो भरे भादों में भी बेरोक-टोक फूलता रहता है। इसी कारण लेखक ने शिरीष निर्धात फूलता है, कहा है।
प्रश्न 2.
किन परिस्थितियों में शिरीष जीवन जीता है?
उत्तर:
चाहे जेठ की चिलचिलाती धूप हो, चाहे पृथ्वी धुयें से रहित अग्नि कुण्ड बनी हो; शिरीष नीचे से ऊपर तक फूल से लदा रहता है। बहुत ही कम पुष्प इस प्रकार की तपती दुपहरी में फूल सकने का साहस जुटा पाते हैं। अमलतास भी शिरीष की तुलना नहीं कर सकता है। इस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी शिरीष जीवन जीता है।
प्रश्न 3.
लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना किससे की है और क्यों ? लेखक के अनुरूप शिरीष के फूलों की क्या प्रकृति है?
उत्तर:
लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना कालजयी अवधूत से की है क्योंकि अवधूत की भाँति ही यह हर परिस्थिति में मस्त रहकर जीवन की अजेयता का सन्देश देता है। शिरीष का फूल एक अवधूत की भाँति दुःख एवं सुख में समान रूप से स्थिर रहकर कभी पराजय स्वीकार नहीं करता है। उसे किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। धरती एवं आसमान के जलते रहने पर भी यह अपना रस खींचता ही रहता है।
प्रश्न 4.
शिरीष के फूलों के सम्बन्ध में तुलसीदास जी का क्या कथन है?
उत्तर:
शिरीष के फूलों के सम्बन्ध में तुलसीदास जी ने कहा है-“धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बताना’ अर्थात् जो फूल फलता है वही अवश्य कुम्हलाकर झड़ जाता है। कुम्हलाने के पश्चात पुनः विकसित हो जाता है।
प्रश्न 5.
लेखक ने शिरीष के सम्बन्ध में किन-किन विद्वानों के नाम बताये हैं?
उत्तर:
लेखक ने शिरीष के सम्बन्ध में कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास तथा आधुनिक काल में अनासक्ति सुमित्रानन्दन पंत एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि विद्वानों के नामों का उल्लेख किया है।
प्रश्न 6.
शिरीष और अमलतास में क्या अन्तर है?
उत्तर:
शिरीष का फूल हर मौसम में फलता फूलता है जबकि अमलतास मात्र पन्द्रह-बीस दिन के लिए फूलता है। बसन्त ऋतु के पलाश पुष्प की भाँति शिरीष का फूल कालजयी एवं अजेय है इस कारण इसकी तुलना अमलतास से नहीं की जा सकती है।
![]()
शिरीष के फूल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। इस वाक्य पर अपने भाव अभिव्यक्त कीजिए।
उत्तर:
जरा (वृद्धावस्था) और मृत्यु ये दोनों ही संसार के चिरपरिचित एवं कटु सत्य हैं। यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध एवं प्रामाणिक है। इसका उल्लेख गीता में भी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के उपरान्त जीव काया रूपी पुराने वस्त्र को त्याग नवीन शरीर धारण करता है। यह क्रम शाश्वत है। किसी कवि ने इस तथ्य को निम्नवत् व्यक्त किया है, देखिए-
“आया है सो जायेगा राजा रंक फकीर”
कोई हाथी चढ़ चल रहा कोई बना जंजीर।”
निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जरा एवं मृत्यु ये दोनों ही तथ्य सत्य हैं इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इस तथ्य को तुलसीदास ने भी स्वीकारा है।
प्रश्न 2.
लेखक ने कबीर की तुलना शिरीष से क्यों की है? समझाइए। (2009)
उत्तर:
लेखक ने कबीर की तुलना शिरीष से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार शिरीष का फूल चाहे गर्मी हो, बरसात हो, बसन्त हो अथवा ग्रीष्म ऋतु की लू के भयंकर थपेड़े हों वह हर दशा में फलता-फूलता है तथा झूम-झूम कर अपनी प्रसन्नता को निरन्तर व्यक्त करता है। शिरीष पर सर्दी, गर्मी, धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जिस प्रकार कबीर अनासक्त योगी थे एवं मस्त-मौजा प्रवृत्ति के संत थे। निन्दा, अपमान अथवा प्रशंसा का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। जैसा कि कबीर के निम्न कथन से यह सत्य उजागर होता है-
“कबिरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ।
जो घर फूंकै आपनो चलै हमारे साथ।।”
लेखक ने शिरीष के फूल को कबीर की भाँति मस्त-मौला एवं मनमौजी प्रवृत्ति का पाया इसी कारण उन्होंने शिरीष की तुलना कबीर से की है और इसे कालजयी एवं अनासक्त अवधूत की संज्ञा प्रदान की।
प्रश्न 3.
कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
कालिदास को अनासक्त योगी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें सम्मान की तनिक भी लालसा नहीं थी। वे सत्ता एवं अधिकार लिप्सा के घोर विरोधी थे। ऐसे व्यक्ति भविष्य में आने वाली पीढ़ी की उपेक्षा को भी सहन कर लेते थे। कालिदास ने अपने शृंगारिक वर्णन में अनासक्त भाव का भली प्रकार विवेचन किया है। वे स्थित प्रज्ञ एवं अनासक्त योगी बनकर कवि सम्राट के आसन पर प्रतिष्ठित हुए। अन्त में कहा जा सकता है जिस प्रकार शिरीष का फूल हर विषम परिस्थिति में फूलता-फलता एवं मुस्कुराता रहता है उसी प्रकार कालिदास भी विषम परिस्थूिति में प्रसन्नतापूर्वक अनासक्त योगी की भाँति अविचल खड़े रहते थे। वास्तव में कालिदास एक सच्चे योगी थे।
प्रश्न 4.
शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुःख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। इस वाक्य के सन्दर्भ में अपने भाव लिखिए। (2008, 09)
उत्तर:
शिरीष का फूल एक अवधूत के समान चाहे दुःख की आँधी हो अथवा सुख की चाँदनी हो वह हर परिस्थिति को समान रूप से ग्रहण करता है। दुःख में कभी हताश नहीं होता तथा सुख में कभी इठलाता नहीं है। वह समान रूप से जीवन जीता है। पराजय स्वीकार करना तो वह जानता नहीं है क्योंकि उसकी धारणा है कि “गति ही जीवन है तथा निष्क्रियता घोर मरण है।”
निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिरीष एक अद्भुत अवधूत की तरह सब कुछ सहन करने के लिए अटल होकर अपने स्थान पर प्रसन्नता से झूमता रहता है। ऋतुओं का क्रम उसको तनिक भी प्रभावित नहीं करता। उसने तो हर परिस्थिति में अवधूत की भाँति मस्त रहना सीखा है। जिस प्रकार अवधूत को सांसारिक भोगों की लिप्सा नहीं रहती है उसी प्रकार शिरीष को भी सर्दी, गर्मी, धूप, छाया की परवाह नहीं रहती है। “प्रसन्नता ही जीवन है”, यही उसके जीवन का मूलमन्त्र है।
प्रश्न 5.
शिरीष जीवन में किस गुण का प्रचार करता है? (2013)
उत्तर:
शिरीष जीवन में इस गुण का प्रचार करता है कि दुनिया के मानव दुःख आने पर क्यों आहें भरता है तथा सुख आने पर गर्व से झूम उठता है। सुख एवं दुःख तो क्रम से आते-जाते रहते हैं। जो मनुष्य आज दुःख की चट्टान के तले दबकर सिसकियाँ ले रहा है कल उसी के कंठ से सुख के स्वर ध्वनित होंगे। इस प्रकार से शिरीष का फूल जीवन में हमें निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सत्ता के मोह और अधिकार के प्रति हम लिप्त न रहें। यह उसका एकमात्र सन्देश है।
जो मानव निरन्तर सत्ता के प्रति लोलुप रहता है, उसका पराभव निश्चित है। धैर्य, साहस एवं तटस्थता जीवन के अपेक्षित गुण हैं जो व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर आरूढ़ करते हैं। शिरीष इन्हीं गुणों का परिचायक है।
![]()
शिरीष के फूल भाषा अध्ययन
प्रश्न 1.
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए
डटे रहना, आँख बचाना, हार न मानना, आँच न आना, न ऊधो का लेना न माधो का देना।
उत्तर:
प्रयोग : (1) डटे रहना – हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पालन के प्रति डटे रहना चाहिए।
(2) आँख बचाना – नौकरानी ने आँख बचाकर मालिक के सारे आभूषण गायब कर दिये।
(3) हार न मानना – उत्साही पुरुष कैसी भी विषम परिस्थिति हो कभी हार नहीं मानते।
(4) आँच न आना – सज्जन ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे उनके चरित्र पर कोई आँच आये।
(5) न ऊधो का लेना न माधो का देना – इस षड्यन्त्र में मधु का कोई हाथ नहीं है उसका तो एकमात्र उद्देश्य है न ऊधो का लेना न माधो का देना।
प्रश्न 2.
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए-
(अ) अशुद्ध – महक उठता है शिरीष का फूल बसन्त के आगमन के साथ।
उत्तर:
शुद्ध – शिरीष का फूल बसन्त के आगमन के साथ महक उठता है।
(आ) अशुद्ध – हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शिरीष के पुष्प मेरे मानस में।
उत्तर:
शुद्ध – शिरीष के पुष्प मेरे मानस में हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं।
(इ) अशुद्ध – छायादार हैं होते बड़े वृक्ष शिरीष के।
उत्तर:
शुद्ध – शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं।
(ई) अशुद्ध – शिरीष का फूल साहित्य में कोमल मानी जाती है।
उत्तर:
शुद्ध – शिरीष का फूल साहित्य में कोमल माना जाता है।
प्रश्न 3.
निम्नलिखित गद्यांश में यथास्थान विरामचिह्नों का प्रयोग कीजिए-
मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी गहराई पर मुहर लगाई थी धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बताना।
उत्तर:
मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती? जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी गहराई पर मुहर लगाई थी, “धरा को प्रमान यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बताना।”
शिरीष के फूल पाठ का सारांश
शिरीष का फूल, साहित्य मनीषी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक सफल एवं उच्च कोटि का प्रेरणादायक निबन्ध है। विद्वान लेखक ने शिरीष के फूल का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है, वह प्रशंसनीय है। शिरीष एक ऐसा फूल है जिसने कालरूपी समय पर विजय प्राप्त कर ली है। वह हर ऋतु में झूमता एवं लहराता रहता है। वह जीवन की अजेय शक्ति का प्रतीक है।
अद्भुत अवधूत की भाँति दुःख एवं सुख को समान रूप से स्वीकार करता है। कबीर तथा आधुनिक काल के सुमित्रानन्दन पन्त एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर भी अनासक्ति भाव से जीवन जीते थे। महात्मा गाँधी भी मार-काट, लूटपाट, रक्त प्रवाह आदि परिस्थितियों में अडिग रहकर धैर्य एवं साहस का परिचय देते थे। अतः उनको भी अवधूत की संज्ञा से विभूषित किया गया है।
![]()
शिरीष के फूल कठिन शब्दार्थ
शिरीष = अति कोमल फूलों वाला एक वृक्ष। धरित्री = धरती। निर्धूम = धुआँ रहित। पलाश = एक प्रकार का लाल रंग का पुष्प। लहक उठता = झूमता। निर्धात अवधूत = सुखदुःख को समान समझने वाला संन्यासी, योगी। कालजयी = जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। मानस = हृदय। हिल्लोल = प्रसन्नता, लहर। अशोक, अरिष्ठ, पुन्नाग और शिरीष = वृक्षों के नाम। मसृण = चिकनी, हरियाली, हरीतिमा। परिवेक्षिष्ठत = घिरी हुई। तुन्दिल = तोंद वाले। पक्षपात = किसी का पक्ष लेना। अधिकार-लिप्सा = अधिकार की लालसा। जीर्ण = पुराने। दुर्बल = कमजोर। परवर्ती = बाद के। ऊर्ध्वमुखी = ऊपर की ओर मुख वाला। ततुंजाल = रेशों का जाल। अनाविल = स्वच्छ, साफ। अनासक्त= आसक्ति रहित। विस्मयविमूढ़ = आश्चर्यचकित। कृषीवल = गन्ने में लगने वाला कीट। कार्पण्य = कंजूस, लोभी। मृणाल = सफेद कमल की डंडी। ईक्षु दण्ड = गन्ना। गन्तव्य = पहुँचने का स्थान। अभ्रभेदी = आकाश को भेदने वाला।
शिरीष के फूल संदर्भ-प्रसंग सहित व्याख्या
1. बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प-पत्र से मर्मरित होती रहती है। शिरीष के पुराने फूल बुरी तरह लड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की याद आती है, जो किसी प्रकार जमाने का साथ नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। (2013)
सन्दर्भ :
प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य-पुस्तक के निबन्ध ‘शिरीष के फूल’ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
प्रसंग :
प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने शिरीष के पुराने फूलों के माध्यम से जमे रहने वाले वृद्ध खुर्रार नेताओं पर कटाक्ष किया गया है।
व्याख्या :
ऋतुराज बसंत के आते ही सारा वन प्रदेश फूल और पत्तों से भर उठता है। पत्तों और फूलों की रगड़ से सरसराहट का स्वर निकलता रहता है, परन्तु शिरीष के पुराने फूल अब तक पेड़ों पर लगे रहते हैं और सूख जाने के कारण परस्पर टकराकर खड़खड़ाहट करते रहते हैं। लेखक को इन फूलों को देखकर उन नेताओं का स्मरण हो उठता है, जो किसी भी तरह समय के परिवर्तन को पहचानने को तैयार नहीं होते हैं। वे राजनीति में जमे ही रहना चाहते हैं। जब नवीन पीढ़ी के नेता उन्हें धकियाकर बाहर कर देते हैं तब बेइज्जत होकर राजनीति से बाहर होते हैं।
विशेष :
- शिरीष के पुराने फूलों के टिके रहने के आधार बनाकर राजनीति में जमे बेशर्म नेताओं पर तीखा प्रहार हुआ है।
- शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।
- विवेचनात्मक शैली अपनाई गई है।
2. मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार-लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती? जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने दुःख के साथ इसकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी,”धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा-सो बताना।” मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा, कि झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। (2011)
सन्दर्भ :
पूर्ववत्।
प्रसंग :
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने वृद्धावस्था एवं मृत्यु को प्रामाणिक सत्य ठहराकर, इस सत्य की तुलना शिरीष के फूल से की है।
व्याख्या :
लेखक का कथन है कि वृद्धावस्था एवं मृत्यु दोनों ही अटल सत्य हैं। इसे कोई भी कदापि असत्य नहीं ठहरा सकता। इतने पर भी मानव अधिकारों के प्रति, प्रतिक्षण लालायित रहता है। उसकी यह आकांक्षा रहती है कि वह अधिक से अधिक अधिकार सम्पन्न बने।
महाकवि तुलसीदास ने इस बात पर वेदना व्यक्त की है और इसकी सत्यता को इस कथन से उजागर किया है-जो फलता-फूलता है वह कुम्हलाकर झड़ भी जाता है। लेखक शिरीष के फूल को देखकर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि पल्लवित एवं पुष्पित होने वाला वृक्ष भी अवश्य ही झड़ता है। काल रूपी देवता निरन्तर बेधड़क कोड़े चला रहा है अर्थात् प्राणी निरन्तर काल-कवलित हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य इस तथ्य को नहीं स्वीकार कर रहा है। जो समय के थपेड़े से जीर्ण-शीर्ण एवं दुर्बल हो चुके हैं, वे धराशायी हो रहे हैं। परन्तु जिनके प्राणों में ऊर्जा शक्ति विद्यमान है वे ही उन्नत रहने में सक्षम हैं।
विशेष :
- जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रामाणिक सत्य हैं।
- भाषा अलंकारिक, परिमार्जित एवं प्रसंगानुकूल है।
![]()
3. शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भाँति मेरे मन में ऐसी अग्नि जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन-धूप, आँधी, लू अपने आप में सत्य नहीं हैं? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार-काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून-खच्चर का बवंडर बह गया है उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है । अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों सम्भव हुआ है? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है और अपने देश का वह बूढ़ा अवधूत था।
(2008)
सन्दर्भ :
पूर्ववत्।
प्रसंग :
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शिरीष के वृक्ष को अवधूत की भाँति स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त मानव को उस वृक्ष से प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश दिया है।
व्याख्या :
लेखक का कथन है कि शिरीष का वृक्ष एक योगी की तरह से हमारे मन-मानस में ऐसी साहस की अग्नि जगा देता है जो हमें सदैव जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चिलचिलाती, धूप, आँधी एवं लू में भी वह सदैव झूमता एवं लहराता रहता है। ये प्रकृति के विभिन्न उपादान जो कि मानव को व्यथित एवं भयभीत करते रहते हैं, लेकिन शिरीष के फूल पर इन बाह्य परिवर्तनों का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे देश में हिंसा, मार-काट, लूट-पाट एवं रक्त-पात का ज्वार सर्वत्र व्याप्त है। परन्तु इस भयावह वातावरण में भारत देश का एक बूढ़ा राष्ट्र नायक शिरीष के फूल की भाँति जीवन में हमें स्थिर रहने का संदेश दे रहा है। गाँधी एवं शिरीष दोनों ही अवधूत की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।
विशेष :
- गाँधी की तुलना शिरीष के फूल से की है। दोनों ही योगी हैं।
- अग्नि जगाना, खून-खच्चर का बवंडर आदि मुहावरों का प्रयोग है।
- भाषा-शैली प्रामाणिक एवं विषयानुरूप है।